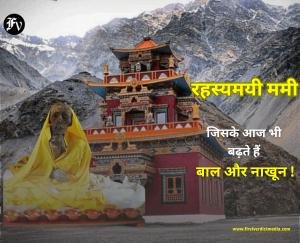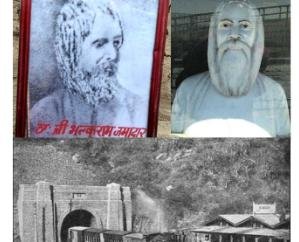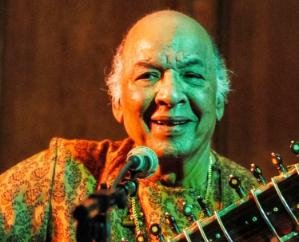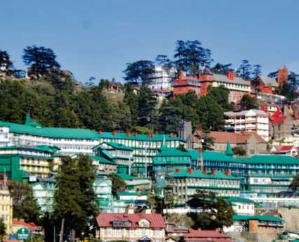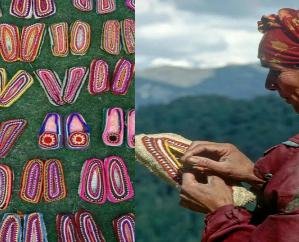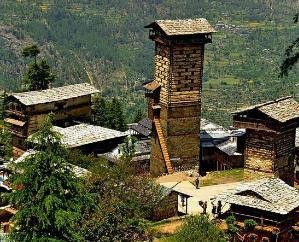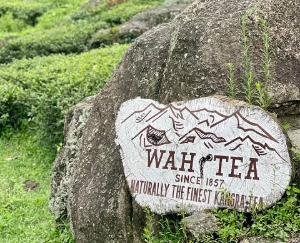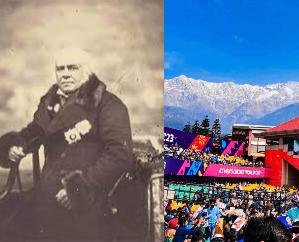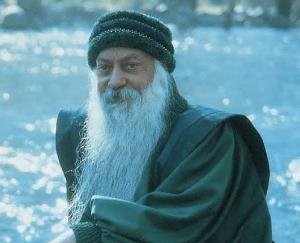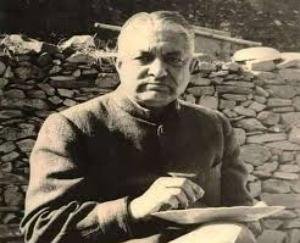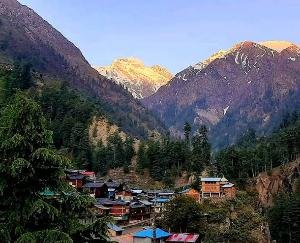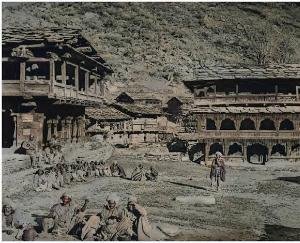हिमाचल प्रदेश एक रहस्यों से भरा राज्य है। यहां ऐसी कई चीज़ें है जिसे समझ पाना वैज्ञानिकों के लिए भी बेहद मुश्किल है। ऐसे ही कई रहस्यों में से एक है हिमाचल की स्पीति घाटी में मौजूद करीब 550 साल पुरानी 'ममी'। करीब 550 साल पुरानी इस 'ममी' को स्थानीय लोग भगवान समझकर पूजते हैं। भारत तिब्बत सीमा पर हिमाचल के लाहौल स्पीति के गयू गांव में मिली इस ममी का रहस्य आज भी बरकरार है। हर साल हजारों लोग इसे देखने के लिए देश विदेश से यहां पहुंचते हैं। यह स्थान हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। लाहौल स्पीति की ऐतिहासिक ताबो मोनेस्ट्री से करीब 50 किमी दूर गयू नाम का यह गांव साल में 6-8 महीने बर्फ से ढके रहने के कारण दुनिया से कटा रहता है। कहते हैं कि यहां मिली यह ममी तिब्बत से गयू गाँव में आकर तपस्या करने वाले लामा संघा तेंजिन की है। कहा जाता है कि लामा ने साधना में लीन होते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तेनजिंग बैठी हुई अवस्था में थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 45 साल थी। इस ममी की वैज्ञानिक जाँच में इसकी उम्र 550 वर्ष से अधिक पाई गई है। आम तौर पर जब भी ममी की बात होती है तो जहन में मिस्र में पाए जाने वाली पट्टियों में लिपटी ममी याद आती है। किसी मृत शरीर को संरक्षित करने के लिए एक खास किस्म का लेप मृत शरीर पर लगाया जाता है, जिससे वह ममी लम्बे समय तक सरंक्षित रहती है। लेकिन इस ममी पर किसी तरह का कोई लेप नहीं लगाया गया है, फिर भी इतने वर्षों से यह ममी सुरक्षित है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ममी के बाल और नाखून आज भी बढ़ते रहते हैं। हालांकि इस तथ्य की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है। इस स्थान पर एक शरीर मौजूद है, जिसके सर बाल है, त्वचा है और नाखून भी पर न तो ये शरीर गलता है और न समय के साथ बदलता है। इसीलिए यहां के स्थानीय लोग इसे जिंदा भगवान मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। बताया जाता है कि ITBP के जवानों को खुदाई के दौरान इस ममी का पता चला था। सन 1975 में भूकंप के बाद एक पुराने मकबरे में ये भिक्षु का ममीकृत शरीर दब गया था। इसकी खुदाई बहुत बाद में 2004 में की गई थी, और तब से यह पुरातत्वविदों और जिज्ञासु यात्रियों के लिए रुचि का विषय रहा है। खुदाई करते वक्त ममी के सर पर कुदाल लग गया था। ममी के सर पर इस ताजा निशान को आज भी देखा जा सकता है। 2009 तक यह ममी ITBP के कैम्पस में रखी हुई थी। देखने वालों की भीड़ देखकर बाद में इस ममी को गाँव में स्थापित किया गया। खास बात यह है कि ममी प्रकृति का प्रकोप झेलने के बावजूद भी सही सलामत है। प्राकृतिक स्व-ममीकरण प्रक्रिया का परिणाम यह ममी मिस्र के ममीकरण से बिल्कुल अलग है। इसे सोकुशिनबुत्सु नामक एक प्राकृतिक स्व-ममीकरण प्रक्रिया का परिणाम कहा जाता है, जो शरीर को उसके वसा और तरल पदार्थ से दूर कर देता है। इसका श्रेय जापान के यामागाटा में बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी की इस प्रक्रिया में दस साल तक लग सकते हैं। इसकी शुरुआत साधु के जौ, चावल और फलियों (शरीर में वसा जोड़ने वाले भोजन) को खाने से रोकने के साथ होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु के बाद वसा यानी फैट सड़ जाती है और इसलिए शरीर से वसा को हटाने से इसे बेहतर तरीके से संरक्षित करने में मदद मिलती है। यह अंगों के आकार को इस हद तक कम करने में भी मदद करता है कि सूखा हुआ शरीर अपघटन का विरोध करता है। शरीर के पास एक निरोधक के साथ-मोमबत्तियां जलाई जाती है ताकि इसे धीरे-धीरे सूखने में मदद मिल सके। शरीर में नमी को खत्म करने और मांस को हड्डी पर संरक्षित करने के लिए एक विशेष आहार भी दिया जाता है। मृत्यु के बाद, भिक्षु को सावधानी से एक भूमिगत कमरे में रखा जाता है। समय के साथ भौतिक रूप सचमुच में एक मूर्ति बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से तीस से भी कम स्व-ममीकृत भिक्षु दुनिया भर में पाए गए हैं। उनमें से अधिकांश जापान के एक द्वीप उत्तरी होंशू में पाए गए हैं। यहां पर भी भिक्षु प्राकृतिक ममीकरण की इस प्रथा का पालन करते हैं। संघा तेनज़िन के शरीर में अवशिष्ट नाइट्रोजन (लंबे समय तक भुखमरी का संकेत) के उच्च स्तर से पता चलता है कि उन्होंने खुद को ममी बनाने के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया था। दांत और बाल आज भी संरक्षित इस ममी के दांत और बाल अभी भी अच्छी तरह से संरक्षित हैं। इस मम्मी को एक छोटे से कमरे में एक कांच के बाड़े में रखा गया है, जो एक लोकप्रिय गोम्पा के करीब स्थित है। इसकी सुरक्षा के लिए इस ममी को एक कमरे में रखा गया है। पर्टयक खिड़की के माध्यम से उसकी एक झलक देख सकते है। इस कमरे को केवल महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान खोला जाता है। गयू आधुनिकीकरण से अछूता एक शांत स्थान है। संघा तेंजिन की ममी आज एक मंदिर में विराजमान है, उसका मुँह खुला है, उसके दाँत दिखाई दे रहे हैं और आँखें खोखली हैं। वसा और नमी से रहित, यह जीवित बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। गाँव के अस्तित्व के लिए दिया था बलिदान मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि संघा तेंजिन ने गाँव के अस्तित्व के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। कहानी यह है कि उन्होंने अपने अनुयायियों से विनाशकारी बिच्छू के संक्रमण के बाद खुद को ममीकृत करने के लिए कहा। जब उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया, तो ऐसा माना जाता है कि क्षितिज पर एक इंद्रधनुष दिखाई दिया जिसके बाद बिच्छू गायब हो गए और प्लेग समाप्त हो गया। सिर्फ 100 लोग बस्ते है इस गांव में गयू गांव एक बेहद शांतिपूर्ण और सुंदर गांव है। इस गांव में लगभग 100 लोग हैं। यहां के निवासी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूर-दूर के स्थानों तक पैदल यात्रा करते हैं। इस गांव की दूरी काज़ा से लगभग 80 किमी है। जबकि शिमला से लगभग 430 किमी और मनाली से कुंजुम दर्रे के माध्यम से इसकी दूरी लगभग 250 किमी है। यहां आने का सबसे सही समय गर्मियों के दौरान है।
नारियल की जगह भैसें को बहाने की थी प्रथा मिंजर मेले की मुख्य शोभायात्रा राजमहल अखंड चंडी से चौगान से होते हुए रावी नदी के किनारे तक पहुंचती है। फिर मिंजर के साथ लाल कपड़े में नारियल लपेट कर, एक रुपया और फल-मिठाई नदी में प्रवाहित किये जाते है। इस नारियल को प्रवाहित करने के पीछे एक रोचक प्रथा है। दरअसल कहा जाता है कि 1940 के दशक कि शुरुआत तक मिंजर मेले में भैंसे की बलि देने की प्रथा थी। तब जीवित भैंसे को नदी में बहा दिया जाता था , जो आने वाले साल में राज्य के भविष्य को दर्शाता था। अगर पानी का बहाव भैंसे को साथ ले जाता था और वह डूबता नहीं था तो उसे अच्छा माना जाता था। अगर भैंसा बच कर नदी के दूसरे किनारे चला जाए, तो उसे भी अच्छा माना जाता था। पर अगर भैंसा उसी तरफ वापस आ जाता था तो उसे बुरा माना जाता था। अब भैंसे की जगह सांकेतिक रूप से नारियल की बलि दी जाती है। पुराने लोगों कि माने तो 19वीं सदी में एक भैंसे ने रावी नदी को पार कर लिया और करीब 17 साल तक यह भैंसा चंबा के राजमहल में बतौर शाही मेहमान रहा। उसकी खातिर के लिए बाकायदा सेवादारों की व्यवस्था भी थी। कहते है उसने लगातार 17 साल तक रावी को पार किया और बाद में राजमहल में उसकी मौत हो गई।
शाहजहां ने मिर्जा साफी बेग को रघुवीर जी के साथ भेजा था राजदूत बनाकर राजा साहिल ने उनकी बेटी राजकुमारी चंपावती के कहने पर रावी नदी के किनारे एक शहर बसाया था, जिसका नाम चंबा रखा गया। महादेव की भूमि इसी चम्बा शहर में हर वर्ष श्रावण माह के दूसरे रविवार को शुरू होता है मिंजर मेला, जो एक सप्ताह तक चलता है। हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, दो समुदायों में एकजुटता की शानदार मिसाल। चंबा के मिर्जा परिवार की ओर से रेशम के धागे में मोती पिरोकर बनाई मिंजर अर्पित की जाती है। इसके बाद अखंड चंडी महल में भगवान रघुवीर को मिंजर चढ़ाई जाती है, एतिहासिक चंबा चौगान (मैदान) में मिंजर का ध्वज चढ़ाया जाता है, और इसके साथ ही मिंजर मेला विधिवत रूप से आरंभ होता है। शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है और फिर पुरे सप्ताह भर चम्बा की बेमिसाल संस्कृति का अद्धभूत मंजर देखने को मिलता है। फिर रावी में मिंजर प्रवाहित कर मेले का समापन किया जाता है। भगवान रघुवीर जी को मिंजर अर्पित करने के पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान सूर्यवंशी राजा पृथ्वी सिंह, रघुवीर जी को चंबा लाए थे। शाहजहां ने मिर्जा साफी बेग को रघुवीर जी के साथ राजदूत के रूप में भेजा था। मिर्जा साहब जरी गोटे के काम में माहिर थे। चंबा पहुंचने पर उन्होंने जरी की मिंजर बनाकर रघुवीर जी, लक्ष्मीनारायण भगवान और राजा पृथ्वी सिंह को भेंट की थी। तबसे परमपरा स्थापित हुई और मिंजर मेले का आगाज मिर्जा साहब के परिवार का वरिष्ठ सदस्य रघुवीर जी को मिंजर भेंट करके करता है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। मिंजर मेले में पहले दिन चंबा के एतिहासिक चौगान तक भगवान रघुवीर जी की शोभायात्रा निकलती है। भगवान रघुवीर जी के साथ आसपास के 200 से अधिक देवी-देवता भी इसमें शामिल होते हैं। मिर्जा परिवार सबसे पहले मिंजर भेंट करता है। पुराने दौरे में इस दौरान घरों में ऋतुगीत और कुंजड़ी-मल्हार गाए जाते थे। पर अब नए दौरे स्थानीय कलाकार मेले में इस परंपरा को निभाते हैं। मिंजर मेले की मुख्य शोभायात्रा राजमहल अखंड चंडी से चौगान से होते हुए रावी नदी के किनारे तक पहुंचती है। यहां मिंजर के साथ लाल कपड़े में नारियल लपेट कर, एक रुपया और फल-मिठाई नदी में प्रवाहित की जाती है। नारियल प्रवाहित करने के पीछे भी रोचक मान्यता है। कहते है पुराने वक्त में भैंसे को नदी में बहाया जाता था। जयराम ठाकुर ने दिया था अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिंजर मेला अब अंतरराष्ट्रीय मेला है। 2022 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मिंजर मेले के समापन पर ये सौगात दी थी। इससे पूर्व चंबा कई बार मिंजर मेला को अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला कहा जाता रहा है, लेकिन सही मायने में मेले को अंतरराष्ट्रीय दर्जा जयराम ठाकुर की सरकार ने दिया। मेले के दौरान जमकर व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। साथ ही सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें चंबा के स्थानीय कलाकारों के अलावा हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के कलाकारों और बालीवुड प्लबैक सिंगर भी पहुंचते हैं। मेले में हाथ से बना सामान काफी बिकता है। चंबा रूमाल, चंबा चप्पल यहां की विशेषता है। इसके अलावा और भी वस्तुओं का व्यापार भी होता है।
अगर कोई प्रेमी जोड़ा देव शंगचूल महादेव की शरण में आ जाए तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। देवता के आशीर्वाद से कई प्रेमी जोड़े सकुशल अपने घरों को लौटे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की सैंज घाटी के शांघड़ गांव में विराजे हैं शंगचूल महादेव, और ये मंदिर घर से भागे प्रेमी जोड़ों के लिए शरणस्थली है। पांडवकालीन शांघड़ गांव में स्थित इस महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि किसी भी जाति-समुदाय के प्रेमी युगल अगर शंगचूल महादेव की सीमा में पहुंच जाते हैं, तो इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहां के लोग प्रेमी जोड़े को मेहमान समझ कर उसका स्वागत करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। शंगचूल महादेव मंदिर की सीमा लगभग 128 बीघा का मैदान है और मान्यता है कि इस सीमा में पहुंचे प्रेमी युगल को देवता की शरण में आया हुआ मान लिया जाता है। इस सीमा में समाज और बिरादरी की रिवाजों को तोड़कर शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए यहां के देवता रक्षक हैं। दिलचस्प बात ये है कि यहां सिर्फ देवता का कानून चलता है। प्रेमी जोड़े, जो मंदिर में आश्रय लेने आते हैं, वह यहां शादी कर सकते हैं और तब तक रह सकते हैं, जब तक प्रेमियों के दोनों तरफ के परिवारों के बीच सुलह नहीं हो जाती। तब तक जोड़े के लिए यहां रहने और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है। इस मंदिर में आने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए पुलिस भी दखलंदाजी नहीं कर सकती। इस मंदिर के पीछे रोचक कहानी है। जनश्रुति के अनुसार, अज्ञातवास के दौरान पांडव यहां रुके थे और उसी दौरान कौरव उनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए। पांडवों ने शंगचूल महादेव की शरण ली और रक्षा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद महादेव ने कौरवों को रोका और कहा कि यह मेरा क्षेत्र है और जो भी मेरी शरण में आएगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महादेव के डर से कौरव वापस लौट गए और इसके बाद से यहां परंपरा शुरू हो गई और यहां आने वाले भक्तों को पूरी सुरक्षा मिलने लगी। शांघड़ पंचायत विश्व धरोहर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क क्षेत्र में होने के कारण भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जंगल की रखवाली करने वाले वन विभाग के कर्मचारियों व पुलिस महकमे के कर्मचारियों को यहाँ अपनी टोपी व पेटी उतारकर मैदान से होकर जाना पड़ता है। देवता का ही फैसला सर्वमान्य शांघड़ गांव में हर नियम और कानून का बेहद सख्ती से पालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस गांव में ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है। इसके साथ ही यहां शराब, सिगरेट और चमड़े का सामान लेकर आना भी मना है। यहां देवता का ही फैसला सर्वमान्य होता है। कहते हैं कि जब तक मामले का निपटारा न हो जाए ब्राह्मण समुदाय के लोग यहां आने वालों की पूरी आवभगत करते हैं और उनके रहने से खाने तक की पूरी जिम्मेदारी यहां के लोग ही उठाते हैं। 128 बीघा में एक भी कंकड़-पत्थर नहीं कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय शांघड़ में भी बिताया और उन्होंने यहां धान की खेती के लिए मिट्टी छानकर खेत तैयार किए थे। वे खेत आज भी विशाल शांघड़ मैदान के रूप में यथावत हैं और इस 128 बीघा में एक भी कंकड़-पत्थर नहीं है और न ही किसी प्रकार की झाड़ियां। वहीं, आधा हिस्सा गौ-चारे के रूप में खाली रखा गया है। यह मैदान अपने चारों ओर देवदार के घने पेड़ों से घिरा है, मानो इसकी सुरक्षा के लिए देवदार के वृक्ष पहरेदार बन खड़े हों। वहीं, मैदान के तीन किनारों पर काष्ठकुणी शैली में बनाए गगनचुंबी मंदिर बेहद दर्शनीय हैं। इस मैदान में शांघड़वासी अपनी गायों को रोज चराते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इस मैदान में गाय का गोबर कहीं भी नहीं मिलता। भूमि की खुदाई, देवता की अनुमति के बगैर नाचना और शराब ले जाने पर भी पाबंदी है। घोड़े के प्रवेश पर भी मनाही शांघड़ गांव में घोड़े के प्रवेश पर भी मनाही है। यदि किसी का घोड़ा शंगचूल देवता के निजी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके मालिक को जुर्माना देना पड़ता है या फिर देवता कमेटी की ओर से उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है।
हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में कई अजीबोगरीब और अद्भुत परंपराएं बसी हुई हैं। इन परंपराओं में से एक है लूण लोटा, जो आज भी पहाड़ी इलाकों में बेहद प्रचलित है। इस प्रथा का पालन करने वाले लोग जब तक अपना वचन या वादा पूरा नहीं करते, तब तक वे किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकते। लूण लोटा का संबंध देवी-देवताओं की अटूट आस्था से है, और यह प्रथा विशेष रूप से उस समय निभाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी बड़े वादे या कसम को निभाने की शपथ लेता है। हिमाचल में यह परंपरा बहुत पुरानी है। जब इन इलाकों में वाद-विवाद सुलझाने के लिए कोई उपयुक्त तरीका नहीं था, तो इस प्रकार की प्रथाएं सामने आईं। पहले यह प्रथाएं शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। समय के साथ, इनका दायरा बढ़ा और चुनावों या अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के संदर्भ में भी इनका इस्तेमाल होने लगा। अर्थात, इन प्रथाओं का प्रारंभ सामाजिक विवादों के निपटारे से हुआ था, लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, इनका उपयोग सत्ता और राजनीति में भी होने लगा। दरअसल लूण का अर्थ है नमक और लोटा वह बर्तन जिसमें पानी होता है। इस प्रथा के दौरान एक व्यक्ति हाथ में पानी से भरे लोटे को पकड़ता है, और दूसरे हाथ से उसमें नमक डालता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने मुंह से एक वचन देता है, जिसे निभाने की वह कसम खाता है। इस वचन के बाद वह शख्स किसी भी हालत में अपने वचन को तोड़ने का नहीं सोचता। नमक और पानी का यह संयोजन एक गहरी सांस्कृतिक आस्था को दिखाता है, जिसमें विश्वास है कि जिस तरह पानी में घुला नमक पूरी तरह से विलीन हो जाता है, वैसे ही वचन तोड़ने से उस व्यक्ति का सम्मान और जीवन खत्म हो सकता है। यह प्रथा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों जैसे शिमला, सिरमौर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में प्रचलित है। शिमला और सिरमौर के आंतरिक इलाकों में इसे लूण लोटा कहा जाता है, जबकि अन्य जगहों पर इसे देवी-देवताओं के नाम पर कसम खिलाने की परंपरा के रूप में देखा जाता है। वोट नोट से नहीं, लूण लोटा से पक्का किया जाता है पंचायत से लेकर लोकसभा तक का चुनाव मतदान के जरिए होता है। चुनाव के दौरान वोट खरीदने के लिए कई उम्मीदवार नोट का सहारा लेते हैं, ये लोकतंत्र का काला सच है। लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में वोट पक्का करने के लिए मतदाताओं को सियासी दलों के कार्यकर्ता लोटे में पानी डालकर कसम दिलवाते हैं। कहा जाता है कि मतदाता वायदे से हट जाएं तो उनको कहीं न कहीं देवता का डर सताता है। यानी लूण लोटा हुआ तो वोट पक्का माना जाता है। गिरीपार और हिमाचल के कुछ इलाकों में इसका ख़ासा इस्तेमाल होता है। ये तरीके भी होते हैं इस्तेमाल लूण लोटा के अलावा हिमाचल प्रदेश में कई और तरीके हैं, जिनके माध्यम से कसम खिलाई जाती है। कुल्लू क्षेत्र में, जहां कश्यप नारायण नामक देवता की पूजा होती है, वहां लोगों को झूठी कसम से बचने के लिए विशेष तौर पर डराया जाता है। इस क्षेत्र में कश्यप नारायण की कसम से लोग बचते हैं, क्योंकि विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति देवता की कसम खाता है और उसे तोड़ता है, तो वह देवता का श्राप पा सकता है। इसी तरह, लाहौल-स्पीति में बौद्ध और हिंदू परंपराओं का समायोजन देखने को मिलता है, जहां कसम दिलाने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है।
हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत में कुछ आयोजन ऐसे हैं, जो केवल पारंपरिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक चेतना और एकता के प्रतीक बन चुके हैं। ऐसे ही एक पावन आयोजन का नाम है भुंडा महायज्ञ। जब यह महायज्ञ होता है, तो पूरा क्षेत्र तीर्थस्थल में परिवर्तित हो जाता है। भुंडा महायज्ञ की उत्पत्ति प्राचीन ग्रंथों, जैसे ब्रह्मांड पुराण और यजुर्वेद से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान परशुराम ने हिमालय की पावन भूमि में व्याप्त राक्षसी शक्तियों का नाश करने के लिए इस यज्ञ की स्थापना की थी। समय के साथ यह यज्ञ नकारात्मक शक्तियों के विनाश, सामाजिक समृद्धि और भाईचारे का प्रतीक बन गया है। स्थानीय जनमानस इसे नरमेज्ञ यज्ञ के रूप में भी जानता है। कई मीटर ऊंचाई से खाई में फिसलता है 'बेड़ा' भुंडा महायज्ञ का दिलकश और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ‘बेड़ा’ अनुष्ठान। आयोजन के तीसरे दिन, एक पुरुष जिसे ‘बेड़ा’ कहा जाता है, विशेष रस्सी (जिसे स्थानीय भाषा में ‘दंड’ या ‘बेरुत’ कहते हैं) पर चढ़कर लगभग कई मीटर ऊंचाई से खाई में फिसलता है। यह रस्सी दो वृक्षों के बीच बंधी होती है और ‘बेड़ा’ उसी पर संतुलन बनाकर यह साहसिक कार्य करता है। कहा जाता है कि यह अनुष्ठान पहले नरबलि के रूप में होता था, लेकिन अब यह केवल प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। यह कर्म लोक भूमि की शुद्धि, बुरी शक्तियों के नाश और सामूहिक बलिदान का अभिव्यक्तिकरण है। 'बेड़ा' करता है कठोर नियमों का पालन, खास घास से बनती है रस्सी कुछ माह पूर्व रोहड़ू के दलगांव में भुंडा महायज्ञ का आयोजन हुआ था। महायज्ञ बेड़ा सूरत राम ने कहा कि, 'वे देवता के मंदिर में पूरे नियम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। आस्था की खाई को पार करने के लिए विशेष घास से खुद रस्सा तैयार किया है। इसे तैयार करने में अपने चार सहयोगियों के साथ करीब ढाई महीने का समय लगा। भुंडा महायज्ञ के लिए बेड़ा को तीन महीने देवता के मंदिर में ही रहना पड़ता है। बेड़ा के लिए एक समय का भोजन मंदिर में ही बनता है। अनुष्ठान के समापन होने तक न तो बाल और न ही नाखून काटे जाते हैं। सुबह चार बजे भोजन करने के बाद फिर अगले दिन सुबह चार बजे भोजन किया जाता है, यानी 24 घंटे में केवल एक बार भोजन किया जाता है। इस दौरान अधिकतम मौन व्रत का पालन किया जाता है। इसके अलावा अन्य प्रतिबंध भी रहते हैं।' बेड़ा सूरत राम ने कहा कि, 'भुंडा महायज्ञ के दौरान बेड़ा रस्सी के जरिए मौत की घाटी को लांघते हैं। ये रस्सी दिव्य होती है और इसे मूंज कहा जाता है। यह विशेष प्रकार की नर्म घास की बनी होती है। इसे खाई के दो सिरों के बीच बांधा जाता है। भुंडा महायज्ञ की रस्सी को बेड़ा खुद तैयार करते हैं।' शिखा फेर, लोकगीत और रात्रि जागरण ‘बेड़ा’ के पहले दिन शिखा फेर का अनुष्ठान संपन्न होता है, जिसमें क्षेत्र की सुरक्षा, सुख-समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। यज्ञ की रात्रियाँ अत्यंत पावन और धार्मिक भाव से ओतप्रोत होती हैं। महिलाएं और बुजुर्ग मिलकर भुंडा और परशुराम की कथाएं गाते हैं, लोकगीतों में देवताओं की महिमा का वर्णन करते हैं, जबकि पुरुष ढोल-नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हैं। यह सामूहिक भक्ति और संस्कृति का सजीव रूप होता है। अंग्रेजों ने लगाया था प्रतिबंध 19वीं सदी में अंग्रेजी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनका मानना था कि इससे इंसानी जान को खतरा होता है, लेकिन आज़ादी के बाद यह प्रथा फिर शुरू हुई, लेकिन अब बेड़ा की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। रस्सी के नीचे नेट (जाली) लगाई जाती है, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान न हो। श्रद्धालुओं की सेवा है लोकपरंपरा की मिसाल कुछ वक्त पूर्व रोहड़ू के दलगांव में भुंडा में लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। भुंडा महायज्ञ के दौरान लगभग 1500 परिवार अपने घरों में 1 लाख से 5 लाख श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। यहाँ कोई व्यावसायिक होटल या निजी व्यवस्था नहीं होती। हर परिवार अपने घर का दरवाजा श्रद्धालुओं के लिए खोलता है, जो ‘अतिथि देवो भवः’ की जीवंत मिसाल है। शुद्ध हिमाचली व्यंजन जैसे चिले, हलवा पूरी, सिड्डू, लोण, चना, शक्करपारे बड़े प्रेम और परंपरा से बनाए जाते हैं। इस महायज्ञ का बजट करीब 100 करोड़ था।
मेनरी मोनेस्ट्री, तिब्बत की मूल आध्यात्मिक बोन परंपरा का मुख्य मठ माना जाता है। पूरी दुनिया में बोन धर्म के अनुयायियों के लिए यह मोनेस्ट्री अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के सोलन-सिरमौर की सीमा पर डोलनजी में स्थित मेनरी मोनेस्ट्री के बारे में हिमाचल में ही बहुत कम लोगों को पता है, किन्तु दुनिया भर में बोन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए इसका सर्वोच्च धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। बोन धर्म तिब्बत की प्राचीन और पारंपरिक धार्मिक प्रथा है। माना जाता है कि लगभग आठवीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म भारत से गया। पर बोन धर्म उससे पहले से ही तिब्बत में प्रचलित था। यानी बोन धर्म तिब्बत का अपना स्थानीय धर्म है। बौद्ध धर्म के तिब्बत में आने के बाद राजकीय समर्थन उस ओर मुड़ गया और बोन धर्म के अनुयायियों के साथ भेदभाव किया जाने लगा, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएँ और कर्मकांड अपना लिए, जिसके चलते यह बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय लगने लगा। जबकि वास्तव में दोनों धर्म अलग-अलग हैं। बोन मतावलंबियों के अनुसार उनका धर्म तोनपा शेनरब द्वारा स्थापित किया गया था, जो शाक्यमुनि गौतम से भी पहले के युग के बुद्ध थे। तिब्बत की मूल आध्यात्मिक परंपरा, बोन परंपरा का मुख्य मठ मेनरी मठ है, जिसकी स्थापना 1405 में न्यामे शेरब ग्यालत्सेन ने की थी। डोलनजी, जो बोन मठ के नाम से भी जाना जाता है, यह मठ चीन द्वारा तिब्बत पर विजय प्राप्त करने के कारण 1967 में डोलनजी में फिर से बनाया गया, और अब यह बोन धर्म की शिक्षाओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह शिक्षा के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता है, जिसमें मेनरी डायलेक्टिक स्कूल आने वाले बोन विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है। यहाँ मौजूद युंगडुंग बोन पुस्तकालय भी दुनियाभर में बोन साहित्य का सबसे बड़ा संग्रह है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बोन धर्म के तत्व सिर्फ तिब्बत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनका ऐतिहासिक प्रभाव तिब्बत से दूर कई मध्य एशिया के क्षेत्रों तक भी मिलता था। इतिहासकार बोन धर्म को तिब्बती साम्राज्य से पहले आने वाले झ़ंगझ़ुंग राज्य से भी संबंधित मानते हैं। जबकि कई विद्वानों का मानना है कि बोन धर्म और हिन्दू धर्म के भगवान शिव में कई तीर्थ और अन्य समानताएँ हैं। मसलन, मानसरोवर और कैलाश पर्वत दोनों ही धर्मों में पवित्र माने जाते थे और हिंदुओं के लिए भगवान शिव के कारण विशेष महत्व रखते हैं। इसी तरह बहुत सी तिब्बत में उत्पन्न होने वाली नदियाँ भी हिंदुओं और बोन धर्मावलंबियों के लिए धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। इसलिए करते हैं जीभ दिखाकर अभिवादन: 18वीं शताब्दी में तिब्बत पर द्जुन्गर कबीलों का कब्जा हो गया। द्जुन्गरों ने स्थानीय धार्मिक परंपराओं का दमन शुरू किया और लामाओं (मोंक्स) और बोन धर्मावलंबियों को जेलों में डाल दिया। उनका मानना था कि लगातार मंत्र पढ़ने से जीभ का रंग काला पड़ जाता है, इसलिए द्जुन्गर अधिकारियों से मिलने आए हर व्यक्ति को अपनी जीभ दिखानी पड़ती थी, ताकि पहचान हो सके कि वह लामा है या नहीं। कालांतर में यह अभिवादन का तरीका बन गया। आज भी तिब्बत में लोग एक-दूसरे को जीभ दिखाकर अभिवादन करते हैं। शिक्षा के बाद मिलती है ‘गेशे’ की उपाधि: डोलनजी स्थित मेनरी विहार बोन धर्म के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ शिक्षा के साथ भिक्षुओं के रहने और खाने का भी प्रबंध होता है। न्यूनतम 12 और अधिकतम 16 वर्ष तक भिक्षुओं को धर्म, दर्शन, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती है। प्रवीणता प्राप्त करने पर भिक्षुओं को ‘गेशे’ की उपाधि मिलती है, जो पीएचडी के समकक्ष मानी जाती है। मौजूदा समय में मोनेस्ट्री में 200 से ज्यादा भिक्षु हैं, जिनमें मंगोलिया, म्यांमार, तिब्बत, नेपाल के भिक्षु भी शामिल हैं।
धौलाधार की ठंडी और ताज़ी हवा के बीच, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में बसा धर्मशाला शहर आज तिब्बती कला और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र बन चुका है। यहाँ स्थापित नॉर्बुलिंका ने न केवल तिब्बती शरणार्थियों की सांस्कृतिक विरासत को संजोया है, बल्कि उसे विश्व स्तर पर पहचान भी दिलाई है। 1980 के दशक की शुरुआत में, तिब्बती धर्म और संस्कृति विभाग के मंत्री कैलसांग येशी और उनकी पत्नी किम येशी ने तिब्बती कला को पुनर्जीवित करने का जो सपना देखा था, वह आज साकार हो चुका है। दशकों के कठिन दौर और विस्थापन के बाद झुकी हुई तिब्बती कला को पुनः उसकी पारंपरिक सुंदरता, गुणवत्ता और उत्कृष्ट कारीगरी के उच्चतम स्तर पर लौटाने के लिए उनका प्रयास निःसंदेह प्रेरणादायक है। दलाई लामा के वित्तीय सहयोग से 1984 में नॉर्बुलिंका के लिए ज़मीन खरीदी गई, और 1988 में जापानी वास्तुकार काज़ुहिरो नाकाहारा के नेतृत्व में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। नाकाहारा ने इस संस्थान को करुणा के देवता ‘अवलोकितेश्वर’ की आकृति में डिज़ाइन किया, जो इसके आध्यात्मिक महत्व को भी दर्शाता है। साल 1995 में, शांति गुरु दलाई लामा ने नॉर्बुलिंका का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थान का हृदय स्थल ‘देदन त्सुकलागखांग’ मंदिर भी पूरा हुआ। यह मंदिर पारंपरिक तिब्बती वास्तुकला और कला का अनूठा नमूना है। मंदिर के अंदर लगी 14 फुट ऊँची स्वर्णित तांबे की बुद्ध प्रतिमा, मास्टर शिल्पकार पेंबा दोर्जे और उनकी टीम की मेहनत और समर्पण की जीवंत मिसाल है। मंदिर की भित्ति चित्रों में भगवान बुद्ध के जीवन के बारह प्रमुख प्रसंगों को चित्रित किया गया है। इसके अलावा, मंदिर की ऊपरी गैलरी में तेरह लामाओं की तस्वीरें तिब्बती इतिहास के गौरवशाली पन्नों को दर्शाती हैं। मंदिर में 16 फुट ऊँचा सिल्क और ब्रॉकेड से बना ‘सोलह अरहतो’ का एप्लीके एक कला का अद्भुत नमूना है, जो महीनों की मेहनत का परिणाम है। नॉर्बुलिंका का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक तिब्बती धार्मिक कला की रक्षा और विकास है। थंगका चित्रकला, लकड़ी की नक्काशी, मूर्तिकला, और थंगका एप्लीके जैसी कलाओं को यहाँ पारंपरिक विधियों से सिखाया जाता है। साथ ही, संस्थान ने आधुनिक डिज़ाइन के क्षेत्र में भी तिब्बती कला को नई पहचान दी है। कपड़े, फर्नीचर, स्क्रीन प्रिंटिंग और होम डेकोर के माध्यम से तिब्बती डिज़ाइन को आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया है। इससे न केवल कला को बढ़ावा मिला है, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित हुई है। नॉर्बुलिंका में तिब्बती भाषा, साहित्य और संस्कृति के अध्ययन के लिए 1997 में एक कॉलेज की स्थापना की गई। यह न केवल कला का केंद्र है, बल्कि तिब्बती संस्कृति के संरक्षण, अध्ययन और शोध का भी प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ युवा तिब्बती छात्र अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हैं, अपनी भाषा और इतिहास से परिचित होते हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान सुदृढ़ होती है। नॉर्बुलिंका सिर्फ कला केंद्र नहीं, बल्कि रोज़गार और सामाजिक विकास का भी आधार है। यह संस्थान कलाकारों और समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हुआ है। संस्थान के आसपास कैफे, दुकानें, रेस्तरां और आवासीय इलाके विकसित हो चुके हैं, जो इसे एक जीवंत सांस्कृतिक हब बनाते हैं। हालांकि संस्थान के पहले मास्टर कलाकार अब नहीं हैं, लेकिन उनके शिष्य उनकी विरासत को संभालते हुए नॉर्बुलिंका की कला को समृद्धि की नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं। बेहद सुंदर है लोसेल डॉल म्यूज़ियम... नॉर्बुलिंका परिसर में स्थित ‘लोसेल डॉल म्यूज़ियम’ तिब्बती जीवन, परिधान और लोककथाओं को रंगीन और जीवंत गुड़ियों के माध्यम से प्रदर्शित करता है। हर गुड़िया हस्तनिर्मित है और तिब्बती संस्कृति की विविधता को दर्शाती है। यह म्यूज़ियम बच्चों, इतिहासकारों और कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। धौलाधार की गोद में बसा नॉर्बुलिंका तिब्बती संस्कृति का वह दीपस्तंभ है, जिसने कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता के माध्यम से अपने लोगों को जोड़े रखा है। यह संस्थान संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मिसाल कायम करता है। नॉर्बुलिंका की कहानी सिर्फ तिब्बती समुदाय की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है, जो अपनी पहचान और विरासत को संजोने का प्रयास करता है।
शिमला के जाखू मंदिर में हनुमान जी के पद चिह्न देखने दुनियाभर से श्रद्धालु आते हैं। प्रकृति की गोद में बसे इस स्थान पर लोगों को बेहद सुकून मिलता है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आते हैं, उन्हें हनुमान जी खाली हाथ नहीं भेजते। शिमला मुख्य शहर से 7 कि.मी. और रिज से दो कि.मी. की दूरी पर स्थित जाखू हिल्स, शिमला की सबसे ऊंची चोटी है और यहीं विराजमान हैं भगवान हनुमान। जाखू मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति देश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है, जो 33 मीटर (108 फीट) ऊंची है। इस मूर्ति के सामने आस-पास लगे बड़े-बड़े पेड़ भी बौने लगते हैं। यह स्थान बजरंगबली के भक्तों के लिए बेहद ख़ास है। पौराणिक कथा के अनुसार: जब श्रीराम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, उस समय लक्ष्मण शक्ति लगने से घायल हो गए थे। उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत पर गए थे। ऐसा कहा जाता है कि संजीवनी लेने जाते समय हनुमान जी कुछ देर के लिए इस स्थान पर रुके थे, जहां अब जाखू मंदिर स्थित है। यह भी माना जाता है कि जब हनुमान जी औषधीय पौधे (संजीवनी) लेने जा रहे थे, तब उन्हें इस स्थान पर ऋषि ‘याक्ष’ (कुछ कथाओं में ‘याकू’) मिले थे। हनुमान जी ने संजीवनी के बारे में जानकारी लेने के लिए यहां विश्राम किया और वापसी में ऋषि से मिलने का वादा किया। लेकिन समय की कमी और दानव कालनेमि के साथ युद्ध के कारण हनुमान जी उस पहाड़ी पर वापस नहीं आ पाए। इसके बाद ऋषि याक्ष ने हनुमान जी के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार, यह मंदिर हनुमान जी के पदचिह्नों के पास बनाया गया है। मंदिर के आस-पास घूमने वाले बंदरों को हनुमान जी का वंशज माना जाता है। माना जाता है कि जाखू मंदिर का निर्माण रामायण काल में हुआ था। इसी स्थान पर प्रकट हुई भगवान की स्वयंभू मूर्ति कथाओं के अनुसार, हिमालय की ओर जाते समय भगवान हनुमान की दृष्टि राम नाम का जाप कर रहे ऋषि याक्ष पर पड़ी। हनुमान जी कुछ देर उनके साथ रुके और विश्राम किया। वापसी के समय उन्होंने ऋषि से भेंट करने का वादा किया, लेकिन देरी होने के कारण वह किसी अन्य मार्ग से निकल गए। ऋषि याक्ष उनके न आने से व्याकुल हो उठे। ऐसी मान्यता है कि तब भगवान हनुमान इस स्थान पर स्वयंभू मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। भगवान हनुमान की चरण पादुका भी है मौजूद जाखू मंदिर में आज भी भगवान हनुमान की स्वयंभू मूर्ति और उनकी चरण पादुका विद्यमान हैं। माना जाता है कि भगवान की स्वयंभू मूर्ति प्रकट होने के बाद ऋषि याक्ष ने ही यहां मंदिर का निर्माण करवाया। ‘याक्ष’ से ‘याकू’ और ‘याकू’ से ही नाम पड़ा ‘जाखू’। मंदिर में स्थापित है 108 फीट ऊंची मूर्ति साल 2010 में जाखू मंदिर में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई, जो शिमला में प्रवेश करते ही दूर से दिखाई देती है। भगवान हनुमान के भक्त रोजाना उनके दर्शन करने यहां पहुंचते हैं, और मान्यता है कि वे अपने सच्चे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं।
हिमाचल के पहाड़ों में कई रहस्य, कई कहानियां छुपी हैं। कुछ कहानियां लोगों तक आसानी से पहुँच जाती हैं और कुछ की तस्वीरें अब भी धुंधली सी हैं। एक ऐसी ही कहानी है बाबा भलकू की। बाबा भलकू वो प्रतिभावान व्यक्ति थे जिन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद भारत-तिब्बत सड़क और कालका-शिमला रेलवे लाइन के निर्माण में अपना अमिट योगदान दिया। बाबा भलकू को कोई इंजीनियर कहता है, कोई संत, तो कोई चरवाहा। बाबा भलकू का जन्म चायल के पास स्थित झाझा गांव के मामूली किसान माठु के घर हुआ था। भलकू बचपन से ही थोड़े अलग थे। उनकी हरकतें आम तौर पर लोगों को समझ नहीं आती थीं, इसीलिए उनके पिता ने उनका बाल विवाह करवा दिया कि शायद वो उसके बाद ठीक हो जाएं। पर विवाह के बाद जो सोचा था, हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। सुधरने की बजाय बाबा भलकू घर छोड़ कर चले गए और कभी नहीं लौटे। भलकू का एक भाई भी था, जावलिया, जिनकी सातवीं पीढ़ी आज भी झाझा गांव में रहती है। ब्रिटिश अधिकारियों ने माना, भलकू की देन है भारत-तिब्बत सड़क बताया जाता है कि घर से भागने के बाद भलकू दर-दर भटकते रहे, कभी साधु-संतों के साथ तो कभी चरवाहों के साथ। कुछ साल बाद भलकू ने पटियाला रियासत के लोक निर्माण विभाग में बतौर मज़दूर काम करना शुरू किया। भलकू ठेठ अनपढ़ होने के बावजूद सड़क निर्माण कार्य में बेहद निपुण थे। अंग्रेज़ भलकू से इतना अधिक प्रभावित थे कि भारत-तिब्बत सड़क निर्माण में भी उनकी सहायता ली गई थी। बाबा भलकू के मार्गदर्शन में न केवल सर्वे हुआ, बल्कि सतलुज नदी पर कई पुलों का निर्माण भी हुआ था। इसके लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा ओवरसियर की उपाधि से नवाज़ा गया था। कहा जाता है कि भलकू अपनी एक छड़ी से नपाई करते और जगह-जगह सिक्के रख देते और उनके पीछे चलते हुए अंग्रेज़ सर्वे का निशान लगाते चलते। टापरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की इंस्पेक्शन बुक में एस. डी. ओ. अंबाला सर्कल बी. एन. आर. ने लिखा है कि भारत-तिब्बत सड़क भलकू जमादार की देन है। भारत-तिब्बत सड़क निर्माण में भलकू के योगदान के बारे में तत्कालीन हिंदुस्तान-तिब्बत रोड के मुख्य अभियंता मेजर ए. एम. लॉन्ग ने 18 अक्टूबर 1875 को फागू बंगले में एक प्रमाण पत्र में लिखा है: "भलकू पिछले 25 वर्षों से हिंदुस्तान-तिब्बत रोड निर्माण कार्य में लगा है। बिना उसके ये कार्य संभव नहीं था। भलकू जैसा प्रतिभावान शायद ही कोई अन्य इस देश में होगा। ऐसी कोई चोटी नहीं जिसे उसने पार नहीं किया। उसके पास नैसर्गिक शक्ति है, जिससे वह सर्वे करते वक्त सही दिशा जान लेता है। इसके साथ ही उसके व्यक्तित्व में न जाने क्या आकर्षण है, मज़दूर उसके इशारे पर जितना काम करते हैं उतना कार्य उनसे कोई नहीं करवा सकता। मेरे हिसाब से भलकू को उनकी सेवा और उनके नायाब उत्साह, बुद्धि और विशेष शक्तियों के लिए विभाग के प्रथम श्रेणी के ओवरसियर के साथ-साथ एक पहाड़ी-सड़क-निर्माता की उपाधि दी जानी चाहिए।" बिन भलकू संभव नहीं था कालका-शिमला रेलमार्ग निर्माण क्या आधिकारिक ब्रिटिश दस्तावेजों में भी है भलकू के योगदान का ज़िक्र? बताया जाता है कि लोक निर्माण विभाग में सेवाएं देने के बाद भलकू की सेवाएं रेलवे में भी ली गईं। बाबा भलकू ने कालका-शिमला रेल मार्ग के निर्माण में भी ब्रिटिश इंजीनियर की सहायता की। कालका-शिमला रेल लाइन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। ब्रिटिश शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को कालका से जोड़ने के लिए 1896 में दिल्ली-अंबाला कंपनी को इस रेलमार्ग के निर्माण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। कहते हैं कि ब्रिटिश काल के कई बड़े-बड़े इंजीनियर्स ने इसे बनाया है, पर जब इस रेल मार्ग को बनाते हुए वे फंस गए तो उन्हें राह दिखाई बाबा भलकू ने। मनमोहक वादियों से गुज़रती देश की सबसे संकरी रेल लाइन बेजोड़ इंजीनियरिंग का जीता-जागता उदाहरण है। इस रेलवे लाइन पर सबसे बड़ी सुरंग नंबर 33, बड़ोग में है जो एक किलोमीटर लंबी है। बड़ोग सुरंग का नाम कर्नल एस. बड़ोग के नाम पर रखा गया है। कालका-शिमला रेलखंड के निर्माण के समय सुरंग संख्या 33 बनाते वक्त अंग्रेज़ इंजीनियर कर्नल बड़ोग सुरंग के छोर मिलाने में असफल हो गए थे। उन दिनों सर्वे का कार्य ज़ोरों पर था। कई दिनों तक लगातार खुदाई करने के बाद जब सुरंग के छोर मिलने का दिन आया, तो पता चला कि 200 मीटर का फासला रह गया है। बड़ोग इस बात से बहुत हताश थे। इस गलती के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कर्नल बड़ोग पर सुरंग के गलत अलाइनमेंट की वजह से हुए नुकसान के लिए एक रुपए का जुर्माना लगाया था। इससे आहत होकर उन्होंने इस सुरंग में आत्महत्या कर ली। कर्नल बड़ोग की मौत के बाद निर्माण की ज़िम्मेदारी मुख्य अभियंता एच. एस. हैरिंगटन को दी गई। बताया जाता है कि एच. एस. हैरिंगटन भी ये कार्य बाबा भलकू की सहायता के बिना पूरा नहीं कर पाते। बता दें कि बड़ोग टनल के बाहर, शिमला में बने बाबा भलकू रेल म्यूज़ियम, बड़ोग स्टेशन और कुछ किताबों में तो बाबा भलकू के रेलवे निर्माण में योगदान का ज़िक्र है, परंतु ब्रिटिश काल के आधिकारिक दस्तावेज़ में बड़ोग टनल के निर्माण का श्रेय बाबा भलकू को दिया गया है या नहीं, इसे लेकर स्पष्टता नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि बाबा भलकू ने ही अंग्रेज़ सरकार से यह दरख्वास्त की थी कि स्टेशन का नाम कर्नल बड़ोग के नाम पर रखा जाए। कहते हैं कि सिर्फ सुरंग नंबर 33 ही नहीं बल्कि सुरंग से आगे बने कई पुल और सुरंगें भी बाबा भलकू ने ही बनाई हैं। तीर्थ पर निकले और फिर लौट कर नहीं आए! बाबा भलकू की सातवीं पीढ़ी से गगनदीप बताते हैं कि बाबा भलकू जिस मकान में रहते थे, वह आज भी उनके गांव झाझा में मौजूद है। वे बताते हैं कि भलकू से अंग्रेज़ों का लगाव बेजोड़ था, वे उन्हें विलायत ले जाना चाहते थे ताकि भलकू की सेवाएं अन्य देशों में भी ली जा सकें। कई बार भलकू के विदेश जाने का प्रबंध भी किया गया लेकिन वे टालते रहे। अंत में वे मान गए लेकिन उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि वे विलायत जाने से पहले तीर्थ करना चाहते हैं। अंग्रेज़ अधिकारियों ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। गगनदीप कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने बताया था कि भलकू तीर्थ पर जाने से पहले सालों बाद अपने पैतृक गांव लौटे। वे गांव तो आए थे पर अपने घर नहीं गए, बल्कि घर के नज़दीक एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लिया। कुछ समय वहां रहने के बाद वे तीर्थ के लिए निकल गए। तीर्थ पर जाने के बाद वे कहां गायब हो गए, किसी को नहीं मालूम। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बाबा भलकू के किस्से केवल किवदंतियों में ही हैं। उत्तर रेलवे भी बाबा भलकू की असल कहानी को सही-सही नहीं जानता। शिमला में बाबा भलकू के नाम से एकमात्र संग्रहालय बना हुआ है। इसमें उनका स्पष्ट विवरण ही अंकित नहीं है।
हिमाचल के एक छोटे से शहर धर्मशाला से एक पूरे देश, यानी तिब्बत की सरकार चलती है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा आज भी भारत में ही रहते हैं। दुनिया भर में दलाई लामा के करोड़ों अनुयायी हैं। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भारत में कदम रखा था। 17 मार्च को वे तिब्बत की राजधानी ल्हासा से पैदल ही निकले थे और हिमालय के पहाड़ों को पार करते हुए करीब 15 दिनों बाद भारतीय सीमा में दाख़िल हुए थे। दलाई लामा के साथ कुछ सैनिक और कैबिनेट के मंत्री थे। चीन की नज़रों से बचने के लिए ये लोग केवल रात को सफर करते थे। महज 23 वर्ष 9 माह की उम्र में जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया, तब देवभूमि हिमाचल के मैक्लोडगंज को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। यहां रहकर वे तिब्बत की संप्रभुता के लिए अहिंसात्मक संघर्ष कर रहे हैं। भारत में दलाई लामा को आए हुए 66 साल से ज़्यादा हो गए हैं। यानी तिब्बत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए आधी सदी से अधिक समय बीत चुका है। संघर्ष का जो रास्ता उन्होंने 23-24 वर्ष की आयु में चुना, उससे वे आजीवन टस से मस नहीं हुए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को तो उन्होंने अपने जीवन में उतार ही लिया था, भारत में आकर महात्मा गांधी के जीवन आदर्श को भी आत्मसात कर लिया। तिब्बत पर चीन के कब्ज़े के ख़िलाफ़ उन्होंने पूरी दुनिया को गोलबंद किया। साथ ही दुनिया भर में फैले तिब्बतियों को एक मंच पर लाया। मौजूदा दलाई लामा को सिर्फ दो साल की उम्र में 13वें दलाई लामा थुबतेन ग्यात्सो का अवतार माना गया और 14वां दलाई लामा घोषित किया गया। उसके बाद वे तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु बने और दुनिया में शांति के आधुनिक प्रतीक के रूप में उभरे। धर्मशाला में निर्वासित जीवन जी रहे वर्तमान दलाई लामा को साल 1937 में उत्तराधिकारी चुना गया था। पूरी तरह तैयार होकर उन्होंने साल 1950 में अपनी जिम्मेदारी संभाली, तब उनकी उम्र मात्र 15 साल थी। 1959 तक दलाई लामा ‘देश के मुखिया’ और सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी थे। कोई उन्हें धर्मगुरु कहता है, कोई शांति का प्रतीक मानता है, तो किसी के लिए वे नेता हैं — सभी की अपनी आस्था और श्रद्धा है। कहा जाता है कि चीन और दलाई लामा का इतिहास, दरअसल, चीन और तिब्बत का इतिहास है। जहां बौद्ध धर्म के लोग दलाई लामा को भगवान का स्वरूप मानते हैं, वहीं चीन उन्हें अलगाववादी मानता है। वह सोचता है कि दलाई लामा उसके लिए समस्या हैं। चीन और दलाई लामा के बीच का विवाद, दलाई लामा की चुनाव प्रक्रिया को लेकर है। दरअसल, 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। लगभग 40 साल बाद चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण तब हुआ जब 14वें दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। कुछ वर्षों बाद तिब्बतियों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वे अपनी संप्रभुता की मांग करने लगे। हालांकि विद्रोहियों को इसमें सफलता नहीं मिली। दलाई लामा को लगा कि वे चीनी चंगुल में फंस जाएंगे, इसीलिए उन्होंने भारत की ओर रुख किया। चीन को भारत में दलाई लामा को शरण मिलना अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओत्से तुंग का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया। दलाई लामा को दुनिया भर से सहानुभूति मिली, लेकिन अब तक वे निर्वासन की ही ज़िंदगी जी रहे हैं। मैक्लोडगंज से चलती है तिब्बत की निर्वासित सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्मशाला में तिब्बती लोगों के रहने के लिए ज़मीन दी। तिब्बतियों को ‘रिफ्यूजी’ का दर्जा दिया गया। कहा जाता है कि उस समय दलाई लामा ने अपने एक अधिकारी को बुलाकर कहा .."धर्मशाला जाओ और पता करो वहां की ज़मीन कैसी है।" कुछ हफ्ते धर्मशाला में रहने के बाद, अधिकारी वापस आया और बोला .. “धर्मशाला का पानी यहां के दूध से भी मीठा है।” यह सुनकर दलाई लामा मुस्कुरा उठे और बोले .. “फिर देर किस बात की, धर्मशाला चलते हैं।” इसके बाद दलाई लामा करीब 80,000 तिब्बतियों के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे और आज भी यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलाई जा रही है। निर्वासित तिब्बत सरकार का बाकायदा चुनाव होता है। चुने गए प्रधानमंत्री को सरलता से सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि हारे हुए प्रतिनिधि भी जीते हुए नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। मान्यता : पुनर्जन्म से मिलते हैं नए दलाई लामा लामा, असल में बौद्ध भिक्षु होते हैं। ये कड़े ध्यान और वर्षों के परिश्रम के बाद जीवन के परम सत्य को जान पाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका कर्तव्य होता है कि वे इस ज्ञान को लोगों के बीच बांटें। इन सभी लामाओं में से दलाई लामा सबसे उच्च पद पर होते हैं। इसे लेकर एक अत्यंत रोचक मान्यता है – जब एक दलाई लामा की मृत्यु होती है, तो वह पुनर्जन्म लेकर दोबारा पृथ्वी पर आते हैं। इसके बाद धार्मिक अधिकारी उस बालक की खोज करते हैं, और फिर उसे ही अगला दलाई लामा घोषित किया जाता है। दलाई लामा को कोई चुनता नहीं, बल्कि उन्हें खोजा जाता है। दलाई लामा का चयन पुनर्जन्म की मान्यता पर आधारित होता है। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद नए लामा की खोज का दायित्व गेलुगपा परंपरा के अनुसार उच्च लामाओं और तिब्बती सरकार का होता है। हालांकि इस खोज में कई वर्ष लग जाते हैं। तिब्बत के वर्तमान 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो को खोजने में 4 वर्षों का समय लगा था। यह खोज दृश्यों और स्वप्नों में मिले संकेतों से शुरू होती है। एक अन्य परंपरा के अनुसार, जब पिछले दलाई लामा को जलाया जाता है, तो उनकी चिता से उठने वाले धुएं को ध्यान से देखा जाता है। माना जाता है कि यह धुआं उनके पुनर्जन्म की दिशा बताता है। इस खोज प्रक्रिया के दौरान उच्च लामा अक्सर केंद्रीय तिब्बत की पवित्र नदी ला-त्सो के पास जाकर ध्यान लगाते हैं।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से न केवल ब्रिटिश राज का इतिहास जुड़ा है बल्कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी शिमला में ही हुई थी। दरअसल, कांग्रेस पार्टी की नींव किसी भारतीय ने न रखकर एक रिटायर्ड अंग्रेज़ अफ़सर ने रखी थी। कांग्रेस पार्टी के जन्मदाता रिटायर्ड अंग्रेज़ अफ़सर ए.ओ. ह्यूम थे। शिमला में रहते हुए ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। आज उनके निवास स्थान को शीशे वाली कोठी के नाम से भी जाना जाता है, जो उस वक्त रोथनी कैसल के नाम से जानी जाती थी। इसलिए रोथनी कैसल का भारतीय इतिहास में एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। कौन थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम मूल रूप से स्कॉटलैंड निवासी, आई.सी.एस. से सेवानिवृत्त भारतीय अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। तब इस पार्टी का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ना नहीं था। कांग्रेस का गठन देश के प्रबुद्ध लोगों को एक मंच पर साथ लाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि देश के लोगों के लिए नीतियों के निर्माण में मदद मिल सके। थियोसोफिकल सोसाइटी के 17 सदस्यों को साथ लेकर ए.ओ. ह्यूम ने पार्टी बनाई। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कहा यह भी जाता है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफ़रिन (1884–1888) ने पार्टी की स्थापना का समर्थन किया था। ए.ओ. ह्यूम को पार्टी के गठन के कई सालों बाद तक भी पार्टी के संस्थापक के नाम से वंचित रहना पड़ा। 1912 में उनकी मृत्यु के पश्चात कांग्रेस ने यह घोषित किया कि ए.ओ. ह्यूम ही इस पार्टी के संस्थापक हैं। 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। 1838 में हुआ था रोथनी कैसल का निर्माण शिमला के जाखू मंदिर को जाने वाले रास्ते पर रोथनी कैसल का निर्माण 1838 में हुआ था। बताया जाता है कि पहले सचिव डॉ. कार्टे ने 1843 में यहां शिमला बैंक कॉरपोरेशन का कार्य शुरू किया था। फिर 1851 में यहां से बैंक को शिफ्ट किया गया। उस समय बैंक के ही एक कर्मचारी आर्नल ने इसे खरीद लिया। इसके बाद यहां ए.ओ. ह्यूम ने अपना आशियाना सजाया। 1867 में ह्यूम ने ही इसका नाम रोथनी कैसल रखा था। बताया जाता है कि भारत सरकार के तत्कालीन सचिव ह्यूम के दिमाग में कांग्रेस को बनाने का विचार भी यहीं पर रहते हुए आया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के संबंध में कई महत्वपूर्ण बैठकों का भी यहां आयोजन हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक हुई थी रोथनी कैसल में भारत सरकार के सचिव रहते हुए ए.ओ. ह्यूम को जब कांग्रेस पार्टी बनाने का ख्याल आया तो रोथनी कैसल में ही वायसराय के साथ अलग-अलग मसलों पर बैठकें भी किया करते थे। वायसराय के कई विशिष्ट अतिथि भी तब ए.ओ. ह्यूम के साथ रोथनी हाउस में ही दिन बिताते थे। बताया जाता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने इसी निजी आवास में की थी और यहीं पर पार्टी की पहली बैठक भी आयोजित की गई थी। ‘अब शीशे वाली कोठी’ के नाम से जाना जाता है शिमला के जाखू स्थित स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के निजी आवास हॉली लॉज से बस कुछ ही दूरी पर रोथनी कैसल स्थित है। मौजूदा समय में इसे शीशे वाली कोठी के नाम से जाना जाता है। इस एक मंज़िला इमारत के निर्माण में शीशे का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। साथ ही इसके निर्माण में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। बताया जाता है कि ए.ओ. ह्यूम के बाद यह लाला छूनामल के वंशजों का आवास रहा है। रोथनी कैसल का अधिग्रहण करना चाहते थे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की सियासत में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह एक बड़ा नाम हैं। वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के विकास में उनका अहम योगदान भी रहा है। वीरभद्र सिंह अपने निजी आवास हॉली लॉज से चंद मीटर की दूरी पर बने रोथनी कैसल का अधिग्रहण करना चाहते थे और इस जगह एक म्यूज़ियम बनाना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के इतिहास को संजोए हुए रोथनी कैसल का अधिग्रहण कर यहाँ म्यूज़ियम बनाने का स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का सपना अधूरा रह गया।
धर्मशाला से करीब 20 किलोमीटर दूर, धौलाधार की तलहटी में बसे खनियारा गांव में स्थित महादेव मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था है। अघंजर महादेव के नाम से प्रसिद्ध इस प्राचीन मंदिर में शिव भक्तों की टोलियां निरंतर पहुंचती हैं। इस स्थान पर 500 वर्षों से बाबा श्री गंगा भारती जी महाराज का अखंड धूणा जल रहा है। माना जाता है कि इसी स्थान पर बाबा ने तपस्या की थी। यूँ तो इस मंदिर में साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन विशेषकर सावन माह और महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ अधिक भीड़ देखने को मिलती है। माना जाता है कि मंदिर की स्थापना महाभारत कालीन है। दंतकथाओं के अनुसार, खनियारा गांव में महाभारत के वन पर्व में अर्जुन ने भगवान शिव से पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। इसी स्थान पर पांडुपुत्र अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण ने भोलेनाथ की उपासना करने को कहा। अर्जुन ने यहीं बैठकर घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान कीं। कहा जाता है कि भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर इसी रास्ते से जाया करते थे और अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया। चट्टान के नीचे स्थित है प्राचीन शिवलिंग मंदिर के समीप बहने वाली मांझी खड्ड के पास एक चट्टान के नीचे प्राचीन शिवलिंग स्थित है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहां दूर-दराज़ से श्रद्धालु पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। पांडवों ने की थी स्थापना राजपाट त्यागने के बाद वनवास के दौरान अर्जुन ने हिमालय यात्रा करते हुए पुनः इसी स्थान पर गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन किए। तत्पश्चात पांडवों ने यहां भगवान शिव का मंदिर अघंजर महादेव नाम से निर्मित किया।मंदिर के पुजारियों के अनुसार, 'अघंजर' का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाला..‘अघ’ का अर्थ है पाप, और ‘अंजर’ का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। महाभारत युद्ध में अपने ही गुरुओं, भाइयों और पूर्वजों का संहार करने के पश्चात पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसी उद्देश्य से अर्जुन के कहने पर इस स्थान पर भगवान शिव के एक और मंदिर की स्थापना की गई। बाबा गंगा भारती जी का इतिहास प्राचीन ऐतिहासिक अघंजर महादेव का इतिहास बाबा गंगा भारती जी, महाराजा रणजीत सिंह, और पांडुपुत्र अर्जुन से जुड़ा हुआ है। मंदिर से जुड़ी अनेक दंतकथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह उदर रोग से पीड़ित थे। जब उन्होंने अपनी व्यथा बाबा गंगा भारती जी को बताई, तो बाबा जी ने तीन चुल्लू पानी पिलाकर उन्हें पूरी तरह ठीक कर दिया। इस पर प्रसन्न होकर महाराजा ने बाबा जी को अपना रेशमी दुशाला भेंट किया।बाबा जी ने वह दुशाला अपने हवन कुंड (धूणे) में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसी धूणे से सैकड़ों एक जैसे दुशाले निकालकर बाबा जी ने कहा—"पहचान कर अपना दुशाला उठा लो।" यह चमत्कार देखकर महाराजा चकित रह गए और बाबा जी की शरण में आ गए। इसके पश्चात महाराजा रणजीत सिंह ने बाबा जी को मंदिर निर्माण हेतु भूमि दान की। यही वह स्थान है जहां बाबा गंगा भारती जी ने जीवित समाधि ली थी। आज मंदिर परिसर में बाबा जी का समाधि स्थल भी स्थित है।
देवभूमि हिमाचल के जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र का पहला पड़ाव है श्री रेणुका जी, जिसे भगवान परशुराम की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ स्थित पवित्र रेणुका झील करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और मान्यता है कि इस झील में भगवान परशुराम की माता रेणुका निवास करती हैं। माता रेणुका के नाम पर ही इस झील और स्थान का नाम पड़ा है। मान्यता है कि दशमी से एक दिन पहले माँ रेणुका अपने पुत्र परशुराम से मिलने यहाँ आती हैं। इस दौरान यहाँ उत्सव मनाया जाता है। पवित्र झील के जल में लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। आस्था से सराबोर रेणुका मेले का आयोजन पांच दिन तक किया जाता है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है और इसे काफी पवित्र भी माना जाता है। कहा जाता है कि झील भगवान परशुराम की माता रेणुका का स्थायी निवास है, जो सदियों से इसी झील में वास कर रही हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक, रेणुका वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु के छठे स्वरूप परशुराम का जन्म हुआ था। कहते हैं, महर्षि जमदाग्नि और उनकी पत्नी भगवती रेणुका जी ने झील के साथ लगती चोटी तापे का टिब्बा में सदियों तक तपस्या की थी। उस समय इस झील का नाम राम सरोवर होता था। भगवान विष्णु ने इनकी तपस्या से खुश होकर वर दिया कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जिसके बाद भगवान परशुराम का जन्म हुआ। पर इसके कई वर्षों बाद सहस्त्रबाहु नाम के एक शक्तिशाली शासक ने इस इलाके पर हमला कर दिया। दरअसल, महर्षि जमदाग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसे हासिल करने के लिए उसने महर्षि जमदाग्नि को भी बंधक बना लिया। किंतु महर्षि जमदाग्नि ने यह कहकर गाय देने से इंकार कर दिया कि यह गाय उन्हें भगवान विष्णु ने दी है। ऐसे में वह इस गाय को किसी और को देकर भगवान का भरोसा नहीं तोड़ सकते। इस पर क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने महर्षि की हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी रेणुका जी साथ लगते राम सरोवर में कूद गईं और हमेशा के लिए जल समाधि ले ली। उक्त घटना के वक्त भगवान परशुराम वहाँ नहीं थे, पर बाद में जब परशुराम को इसका पता चला तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। साथ ही तपस्या से पिता को भी नया जीवन दे दिया। परशुराम ने अपनी माता रेणुका से विनती की कि वे झील से बाहर आएं, मगर माँ रेणुका ने कहा कि वे अब हमेशा के लिए इस झील में वास करेंगी, पर वे परशुराम से मिलने साल में एक बार आएंगी। इसके बाद ही झील का नाम रेणुका झील पड़ा और उसी समय से इसकी आकृति भी महिला के आकार में ढल गई। मान्यता है कि दशमी से एक दिन पहले माँ परशुराम से मिलने आती हैं। कोई नहीं माप पाया झील की गहराई: भगवान परशुराम की जन्मभूमि श्री रेणुका जी उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में से एक है। रेणुका जी झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और लगभग तीन किलोमीटर में फैली है। खास बात ये है कि इस झील का आकार स्त्री जैसा है और इसे माता रेणुका की प्रतिछाया माना जाता है। कहते हैं कि कई बार वैज्ञानिकों ने इस झील की गहराई को मापने की कोशिश की, मगर वे इस काम में सफल नहीं हो सके।
आजादी के बाद, साल 1947 से लेकर 1956 तक पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस सोलन में था। ब्रिटिश हुकूमत के जाने के बाद सोलन का कैंटोनमेंट एरिया खाली था और वहीं करीब नौ साल पंजाब यूनिवर्सिटी चली। यह क्षेत्र करीब आठ किलोमीटर में फैला था। दरअसल, पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना 1882 में लाहौर में हुई थी और यह ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत में खोली गई चौथी यूनिवर्सिटी थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त यूनिवर्सिटी का भी विभाजन हुआ और इसे दो भागों में बाँट दिया गया; यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को कुछ सालों के लिए सोलन के कैंटोनमेंट एरिया में स्थापित किया गया। फिर 1956 से इसे चंडीगढ़ शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया। 1958 से 1960 के बीच में चंडीगढ़ स्थित मौजूदा कैंपस बनकर पूरी तरह तैयार हो रहा था और तब से पंजाब यूनिवर्सिटी इसी कैंपस से चल रही है। 1966 में पंजाब के पुनर्गठन होने तक पंजाब यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर रोहतक, शिमला और जालंधर में चलते रहे। वहीं, 1971 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने से पहले हिमाचल के कई कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहे।
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित जटोली शिव मंदिर को एशिया का सबसे ऊँचा शिव मंदिर माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 1,855 मीटर (करीब 6,086 फीट) की ऊँचाई पर स्थित यह मंदिर अपने स्थापत्य, धार्मिक महत्त्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। स्थान और पहुँच जटोली मंदिर, सोलन शहर से लगभग छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सड़क मार्ग से यहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के निकट तक वाहन सुविधा उपलब्ध है। स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस मंदिर की स्थापना का श्रेय श्रीश्री 1008 स्वामी कृष्णा नंद परमहंस महाराज को जाता है, जो वर्ष 1946 में इस क्षेत्र में आए थे। उस समय यह स्थान एक घना जंगल हुआ करता था। परमहंस महाराज को यह स्थान तपस्या के लिए उपयुक्त प्रतीत हुआ, और उन्होंने यहाँ रहकर साधना आरंभ की। दिन में वह कुंड के पास ध्यान करते और रात को एक गुफा में विश्राम करते थे। समय के साथ स्थानीय लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए परमहंस महाराज ने भगवान शिव की आराधना करते हुए जलधारा के लिए तप किया। कुछ ही समय बाद मंदिर परिसर में एक जलधारा फूट पड़ी, जो आज भी 'शिव कुंड' के रूप में निरंतर बहती है। निर्माण और वास्तुकला जटोली शिव मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 1980 में प्रारंभ हुआ। इसे दक्षिण भारत की द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया है। मंदिर के निर्माण में लगभग 33 वर्ष का समय लगा और इसे वर्ष 2013 में आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। मंदिर की शिखर ऊँचाई लगभग 122 फीट है, जिससे यह एशिया का सबसे ऊँचा शिव मंदिर माना जाता है। निर्माण कार्य में पारंपरिक पत्थरों, लकड़ी और आधुनिक तकनीकों का समन्वय किया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारों और स्तंभों पर बारीक नक्काशी की गई है, जो इसकी शिल्पकला की श्रेष्ठता को दर्शाती है। मंदिर की विशेषताएँ तीन मंजिला संरचना: मंदिर तीन स्तरों पर बना है। प्रथम तल पर शिवलिंग और जल कुंड, द्वितीय तल पर ध्यान कक्ष, और तृतीय तल पर मुख्य शिखर स्थित है। शिव कुंड: परिसर में मौजूद जलधारा से निर्मित यह कुंड एक प्रमुख आकर्षण है। इसका पानी साल भर बहता रहता है और इसे पवित्र माना जाता है। आसपास का वातावरण: मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों और देवदार के वृक्षों से घिरा है, जो इसे एक शांत और ध्यानयोग्य स्थल बनाता है। धार्मिक आयोजन: महाशिवरात्रि, श्रावण मास और अन्य शिवोत्सवों पर यहाँ विशेष पूजा-अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। वर्तमान स्थिति और सामाजिक योगदान आज जटोली मंदिर हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। यह न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी प्रोत्साहित कर रहा है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया जाता है। मंदिर परिसर में जल, स्वच्छता और यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं की उचित व्यवस्था की गई है।
जब शहरों की चकाचौंध थमती है, और प्रकृति अपने मौन संगीत में लिपटी होती है, तब हिमाचल के शांत और ऊँचे पहाड़ी क्षेत्र वह ख़ामोश मंच बन जाते हैं जहाँ रात का आसमान खुलकर अपनी कहानियाँ कहता है। टिमटिमाते तारे, आकाशगंगा की चमकती धाराएँ और ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य, ये सब कुछ खुली आँखों से देखने का सौभाग्य बहुत कम जगहों पर मिलता है, और हिमाचल उनमें सबसे ऊपर है। देवभूमि अब ‘स्टारगैज़िंग’ यानी तारों को निहारने की अद्भुत कला के लिए खगोल प्रेमियों का नया तीर्थ बन रहा है। यहाँ की पर्वतीय रातें सिर्फ ठंडी नहीं होतीं, वे ब्रह्मांड का खुला द्वार बन जाती हैं। यही नहीं, स्पीति घाटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स (Indian Institute of Astrophysics – IIA) ने अंतरिक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में मान्यता दी है। यह घाटी खगोलीय वेधशाला के लिए एक आदर्श स्थान है क्योंकि यहाँ की मौसम की स्थिति, उच्च ऊँचाई और कम प्रदूषण वाले वातावरण के कारण आकाश को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्टारगैज़िंग, यानी तारों को ध्यानपूर्वक देखना और उनका अनुभव लेना, केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। इसमें हम तारों की चाल, उनके समूहों, आकाशगंगा और ग्रहों का अवलोकन करते हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल ब्रह्मांड को देखने, बल्कि उसमें अपनी जगह को समझने का अवसर देती है। आजकल स्टारगैज़िंग को खगोल पर्यटन (Astro Tourism) के रूप में बढ़ावा मिल रहा है, जहाँ लोग रातभर खुले आसमान के नीचे तारे देखना, उन्हें कैमरे में क़ैद करना और ब्रह्मांड से जुड़ना पसंद कर रहे हैं। स्पीति: जहाँ रातें सितारों से बातें करती हैं लाहौल-स्पीति ज़िला, विशेषकर काजा, हिक्किम, लांगज़ा और किब्बर जैसे गाँव, आज देश-विदेश के खगोलप्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। इन गाँवों की ख़ासियत है .. वातावरण की नमी लगभग शून्य होना, अत्यधिक ऊँचाई और नगण्य प्रकाश प्रदूषण। ऐसे में यहाँ का आसमान रात के समय आकाशगंगा (Milky Way), प्लेइडीज़, ओरायन बेल्ट और कभी-कभी उल्कापिंडों (shooting stars) से सजा नज़र आता है। हिक्किम का डाकघर, जो दुनिया का सबसे ऊँचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस है, अब ‘स्टारगैज़िंग पोस्ट’ के रूप में लोकप्रिय होता जा रहा है। चंद्रताल: ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करती झील समुद्र तल से 14,100 फीट की ऊँचाई पर बसी चंद्रताल झील, अपने अर्धचंद्राकार आकार और दर्पण-सी शांति के कारण प्रसिद्ध है। रात को जब पूरा ब्रह्मांड इस झील की सतह पर प्रतिबिंबित होता है, तो वह दृश्य अविस्मरणीय होता है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता, लेकिन सितारों से कनेक्शन की ऐसी स्थायी रेखा बनती है, जो हर स्क्रीन से कहीं ज़्यादा गहरी और शुद्ध होती है। छितकुल और ट्रियुंड: जहाँ तारे ज़मीन से उतरते हैं किन्नौर का छितकुल — यानी भारत का आख़िरी गाँव — अब स्टारगैज़िंग के लिए एक शांत और सुंदर विकल्प बनकर उभरा है। यहाँ के खुले मैदानों से आकाशगंगा को निहारना आत्मा के लिए ध्यान जैसा अनुभव देता है। वहीं धर्मशाला के पास ट्रियुंड ट्रेकिंग पॉइंट पर अगर आप एक रात टेंट में बिताएँ, तो आपको तारे ज़मीन पर उतरते हुए महसूस होंगे। इसके अलावा, नाको (किन्नौर), करज़ोक (त्सो मोरीरी के पास), केलांग (लाहौल), भरमौर (चंबा), और रोहतांग दर्रे के आसपास के क्षेत्र भी स्टारगैज़िंग के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। इन क्षेत्रों में ट्रैकिंग और खगोल पर्यटन को जोड़कर स्थानीय लोगों ने ‘एस्ट्रो होमस्टे’ जैसी पहल भी शुरू की है। स्टारगैज़िंग के लिए एक स्पष्ट रात, बिना चाँद की रातें (अमावस्या), ऊँचाई वाला क्षेत्र, कम रोशनी वाला वातावरण, और अधीरता से दूर एक शांत मन बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग स्टार मैप ऐप्स या दूरबीन का सहारा लेते हैं, जबकि कुछ बस खुली आँखों से इस अलौकिक दृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहते हैं। हिमाचल में इसका आदर्श समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक होता है। स्टारगैज़िंग ने खोले रोज़गार के द्वार घाटी और आसपास के इलाक़ों में स्टारगैज़िंग रोज़गार का ज़रिया बनता जा रहा है। जैसे-जैसे स्टारगैज़िंग डॉक्यूमेंट्री और प्रोफेशनल टाइमलैप्स वीडियो की माँग बढ़ रही है, वैसे-वैसे स्थानीय लोगों की भूमिका भी अहम होती जा रही है। एक पेशेवर खगोलीय वीडियो शूट की क़ीमत लाखों में होती है। इसमें हाई-एंड कैमरा, ड्रोन, लोकेशन शूट, टीम खर्च और एडिटिंग शामिल होते हैं। अब बाहरी शूटिंग टीमें जब इन दूरदराज़ घाटियों में आती हैं, तो स्थानीय लोग उन्हें गाइड, पोर्टर, टैक्सी ड्राइवर, होमस्टे और खानपान की सेवाएँ देते हैं। इससे उनकी आमदनी में सीधा इज़ाफा हो रहा है।
"डगशाई जेल की दीवारें मानो आज भी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी कह रही हों। जेल में बनी कालकोठरी बेहद भयानक है, यहाँ का घुप अंधेरा आज भी शरीर में सिरहन ला देता है। ब्रिटिश शासन में इस जेल में न जाने कितने कैदियों को प्रताड़ित किया जाता था। न जाने कितने आज़ादी के मतवालों को यहाँ अमानवीय दंड दिए गए। यहाँ कैदियों के माथे को गर्म सलाखों से दागा जाता था। इसलिए इसे 'दाग-ए-शाही' सज़ा कहा जाता था। 'दाग-ए-शाही' नाम से ही दागशाई नाम की उत्पत्ति हुई और फिर इसे डगशाई कहा जाने लगा।" हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले की डगशाई जेल के साथ एक अनूठा इतिहास जुड़ा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस जेल में दो दिन बिताए थे। गांधी आयरिश नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद आयरिश कैदियों से मिलने आए थे। गांधीजी की यात्रा के दौरान अंग्रेजों ने उनके रहने की व्यवस्था कैंटोनमेंट इलाके में की थी, लेकिन उन्होंने डगशाई जेल में ही रहने की मांग की थी। दिलचस्प बात ये है कि बापू के हत्यारे गोडसे इस जेल का आख़िरी कैदी था। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को शिमला में ट्रायल के दौरान डगशाई जेल लाया गया था। गोडसे को जेल के मुख्य द्वार के प्रवेश द्वार के बगल वाली कोठरी नंबर छह में रखा गया था, जहाँ आज भी दीवार पर गोडसे की फोटो टंगी हुई है। डगशाई जेल अब म्यूज़ियम बन गई है। महात्मा गांधी जिस कोठरी में रुके थे, वहाँ आज भी गांधीजी की एक तस्वीर, एक चरखा और एक गद्दा रखा हुआ है। आज भी हज़ारों लोग इस जेल को देखने आते हैं। जेल म्यूज़ियम में घूमने से आज़ादी से पहले के काले इतिहास को क़रीब से जाना जा सकता है। ब्रिटिश शासन में इस जेल में कैदी को जेल की कोठरी के दो दरवाज़ों के बीच खड़ा किया जाता था। दोनों दरवाज़ों को बंद करने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता था कि कैदी कई घंटों तक बिना आराम किए इन दो दरवाज़ों के बीच रहे। इस जेल में कैदी का एक कार्ड भी बनाया जाता था। इस कार्ड में कैदी का पूरा विवरण लिखा होता था, जिसमें उसका नाम, रंग, देश, अपराध, कारावास की अवधि और फ़ैसले की तारीख़ शामिल होती थी।
"जब भी भारत के लोग राष्ट्रगान की धुन सुनकर सावधान खड़े होते हैं, तो हमें इसे कलमबद्ध करने वाले रवीन्द्रनाथ टैगोर ज़ेहन में आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि हमारे राष्ट्रगान 'जन गण मन...' की धुन हिमाचल प्रदेश में जन्मे एक गोरखा राम सिंह ठाकुर ने तैयार की थी। ये हर हिमाचली के लिए गौरव का संदर्भ है।" "आज़ादी के मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर कैप्टन राम सिंह के नेतृत्व में INA (इंडियन नेशनल आर्मी) के ऑर्केस्ट्रा ने लाल क़िले पर 'शुभ सुख चैन की बरखा बरसे...' गीत की धुन बजाई थी।" नेता जी ने दिया था अपना वायलिन आज़ाद हिंद फ़ौज में रहते हुए जब कैप्टन राम सिंह की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पहली बार मुलाक़ात हुई, तो उन्होंने उनके सम्मान में मुमताज़ हुसैन के लिखे एक गीत को अपनी धुन देकर तैयार किया। ये गीत था... 'सुभाष जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए'। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अपना पसंदीदा वायलिन उपहार में दिया और राम सिंह को ये ज़िम्मेदारी दी कि वह ऐसे गीत बनाएं जो उनकी सेना का हौसला बनाए रखें और देशवासियों के दिलों में जोश भर दें। 2002 में हुआ देहांत, हिमाचल में उपेक्षित और गुमनाम सेना से रिटायरमेंट के बाद यूपी सरकार ने सम्मान के तौर पर उन्हें पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैप्टन राम सिंह को आजीवन लखनऊ में ही रहने के लिए बंगला आवंटित किया था। 2002 में कैप्टन राम सिंह ने लखनऊ में ही अंतिम सांस ली। पर ये विडंबना का विषय है कि आज मौजूदा वक्त में राष्ट्रगान की धुन के रचयिता अपने ही प्रदेश हिमाचल में उपेक्षित और गुमनाम हैं।
स्पीति की बर्फ से ढकी चोटियों और घाटियों के बीच बसा हुआ काकती एक ऐसा गांव है, जो न सिर्फ अपनी असाधारण भौगोलिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके अस्तित्व का एक दिलचस्प और अनूठा पहलू है। यह गांव सिर्फ एक घर का है, और यह तथ्य इस गांव की पहचान बन चुका है। काजा पंचायत के अंतर्गत आने वाला यह गांव काजा से लगभग 10 किलोमीटर दूर और 22 घुमावदार मोड़ों के पार स्थित है। एक अद्भुत और आकर्षक जगह है, जो पूरी तरह से एक परिवार की संरचना में समाहित है। हालाँकि कागज़ों में यह गांव 15 बीघा में फैला है। काकती गांव का दिल उस एक घर में बसा हुआ है, जो लगभग 300 साल पुराना है। आज भी, इस घर में छेरिंग नामग्याल का परिवार निवास करता है, जो इस परिवार के पांचवी पीढ़ी है और इस गांव की देखभाल कर रहे हैं। काकती के इस घर की बनावट हिमालय की पारंपरिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह घर मिट्टी और पत्थर से बना पारंपरिक मड हाउस है, जो लगभग 300 साल पुराना है। मड हाउस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में काफी आरामदायक रहता है। सर्दियों में यह घर अंदर से गरम रहता है और गर्मियों में ठंडा। हिमालय की कठोर सर्दी में घर को गर्म रखने के लिए छेरिंग और उनके परिवार सदस्य लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले से ही सर्दियों के लिए लकड़ी जमा कर लेते हैं और घर को गर्म रखने के लिए उसे जलाते हैं। इसके अलावा, घर के भीतर राशन का पर्याप्त भंडारण किया जाता है, ताकि सर्दी में किसी प्रकार की खाद्य सामग्री की कमी न हो। मिट्टी के घर की संरचना इतनी मजबूत है कि यह आसानी से मरम्मत भी की जा सकती है। समय-समय पर इसे नवीनीकरण किया जाता है, ताकि घर की दीवारें और छतें सुरक्षित और टिकाऊ बनी रहें। घर का डिज़ाइन मौसम की परिस्थितियों के अनुरूप है और इसे सर्दी और गर्मी दोनों में आरामदायक बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। छेरिंग नामग्याल कहते हैं, “उनके पूर्वजों ने इस घर को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि यह ठंडे और गर्म मौसम में दोनों में आरामदायक रहे। हमारे लिए यह घर केवल एक आश्रय नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है।" पूर्वज रहते थे चट्टान के नीचे काकती गांव में नामग्याल के घर से कुछ दूरी पर एक सुरंग है , जो लगभग 300 साल पुरानी है। सुरंग उस समय की जीवनशैली की गवाह है, जब इस परिवार का कोई अन्य आवासीय स्थान नहीं था। यह सुरंग न केवल एक शरण स्थल थी, बल्कि परिवार के लिए यह एक जीवन रक्षक स्थान भी साबित हुई थी। हिमालय की कठोर सर्दियों में, जब तापमान -25 डिग्री तक गिर जाता था, तो परिवार के सदस्य यहां आकर शरण लेते थे। सुरंग के अंदर आग जलाकर ठंड से बचाव किया जाता था, और अनाज का भंडारण भी यहीं किया जाता था, ताकि विपरीत मौसम में खाने-पीने की कोई कमी न हो। आज भी अनाज स्टोर करने के साक्ष्य यहाँ मौजूद है। आज भी इस सुरंग में पूजा करने के निशान और धार्मिक उपकरण मौजूद हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह स्थान सिर्फ एक शरण नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थल भी था। समय के साथ, घर बनने के बाद भी इस सुरंग को संरक्षित किया गया है, और यह परिवार के इतिहास, परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा बनी हुई है। स्नो लैपर्ड से डरना क्या काकती के आसपास हिमालयी बाघ या स्नो लेपर्ड (Snow Leopard) का आना-जाना रहता है। इन जंगली जानवरों की आवाजाही इस क्षेत्र में सामान्य बात है, लेकिन छेरिंग नामग्याल और उनका परिवार इन खतरों से बिलकुल नहीं डरते। छेरिंग कहते हैं, "यह हमारा घर है, हम यहाँ जन्मे हैं और यहीं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। जानवरों से क्या डरना। यह साहस और धैर्य इस परिवार की हिमालय की कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की अद्भुत क्षमता को दिखाता है। इस घर और परिवार का साहस हिमालय की कठिनाइयों के खिलाफ उनके संघर्ष की कहानी बयां करता है। आधुनिकता से लैस एक घर काकती में सिर्फ एक ही घर है, बावजूद इसके यह आधुनिकता से भी लैस है। भारत सरकार ने इस दूर-दराज़ और कठिन इलाके में सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की है। BSNL द्वारा 4G मोबाइल नेटवर्क टावर भी यहाँ लगाया गया है, जिससे परिवार और आसपास के लोग इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। छेरिंग कहते हैं, "पहले खबरें हमारे पास हफ्तों बाद आती थीं, अब इंटरनेट और मोबाइल से हम डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं। दुनिया में हो क्या रहा है हमको पता चल जाता है। " काश कोई और परिवार होता ! काकती में सिर्फ एक ही घर है, लेकिन छेरिंग नामग्याल और उनका परिवार चाहते हैं कि यहां एक और घर हो, ताकि उनका परिवार एक साथ रह सके। वे कहते हैं, "हमारा परिवार छोटा है। अगर एक और घर होता तो हम साथ रहते, खुश रहते और एक-दूसरे का सहारा होते। पहाड़ों की इस कठिन ज़िंदगी में साथ होना बहुत जरूरी है। बचपन में कोई आसपास नहीं होता था तो दिन नहीं कटते थे धीरे धीरे आदत बन गयी और अब तो हम बूढ़े भी हो गए। "
ब्रिटिशों की समर कैपिटल रहे शिमला में कई ऐतिहासिक इमारतें और स्थान है। इन्हीं स्थानों में एक स्थान है रिज मैदान का टका बेंच है। इस स्थान का नाम टका बेंच पड़ने की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल ब्रिटिश काल के दौरान शिमला के रिज मैदान और मालरोड सहित कई स्थानों में अश्वेत लोगों का प्रवेश वर्जित था। रिज मैदान के ऊपर एक बेंच हुआ करती थी, जहां अंग्रेजों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के बैठने पर एक टका लिया जाता था। इसी कारण आगे चल कर इस स्थान का नाम टका बेंच के नाम से मशहूर हो गया। टका बेंच कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शिमला की सर्द हवाओं और हल्की बर्फबारी के बीच इसी टका बेंच से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी। साथ ही कई मुख्यमंत्री और मंत्री भी यहीं से अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके है।
सिर्फ 1 रुपये प्रति वर्ष की राजसी राशि पर डॉ परमार ने करवाया था उपलब्ध हिन्दुस्तान के सबसे उम्दा सितार वादकों में शुमार उस्ताद विलायत खान का शिमला से एक अटूट नाता रहा है। 1960 के दशक के मध्य में, वे राजा पदमजीत सिंह के मेहमान के रूप में शिमला आए थे। उस्ताद विलायत खान कुछ वक्त स्ट्रॉबेरी हिल में रहे और फिर उन्होंने छोटा शिमला में ऐरा होल्मे कॉटेज किराए पर लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ वाईएस परमार को इल्म था कि उस्ताद विलायत खान सरीखे कलाकार का शिमला में यूँ रहना कितना ख़ास था, सो उन्होंने उस्ताद को शिमला में रहने के लिए मनाने का फैसला किया। तब उन्हें जुब्बल के राजा के महलों में से एक, परिमहल, किराए पर उपलब्ध करवाया गया, वो भी सिर्फ 1 रुपये प्रति वर्ष की राजसी राशि पर। हिमाचल के साथ उनका एक और जुड़ाव था। दरअसल उनके नाम उस्ताद बंदे हसन खान कुछ सालों तक नाहन में दरबारी संगीतकार थे। उनके पिता के जल्दी देहांत के बाद उन्होंने अपने नाना और मामा से सितार बजाना सीखा था। कहते है उस्ताद विलायत खान पोकर खेलने के शौक़ीन थे। फुर्सत में वे अपने दोस्तों के साथ संगीत और पोकर का आनंद लेते।शिमला के पुराने लोगों को उनकी कोबाल्ट-नीली मर्सिडीज अब भी याद है , जो अफ़गानिस्तान के राजा ने उन्हें उपहार में दी थी। उस दौरान कई शिष्य उनसे संगीत सीखने के लिए शिमला आते थे। कहते है उस दौरे में बनारस घराने के प्रसिद्ध कलाकार पंडित समता प्रसाद भी शिमला आए थे और आइरा होल्मे कॉटेज में उस्ताद विलायत खान के पास रुके थे। उस्ताद विलायत खान 1960 के दशक के अंत में कुछ वर्षों तक शिमला में ही रहे। तदोपरांत पारिवारिक कारणों से वे देहरादून और फिर अमेरिका जा बसे। जाते समय सिर्फ 1 रुपये प्रति वर्ष की राजसी राशि पर मिला परिमहल उन्होंने हिमाचल सरकार को लौटा दिया। अद्भुत है परिमहल, अब यहाँ सरकारी कार्यालय है जिस परिमहल में उस्ताद विलायत खान रहते थे उसका संबंध जुब्बल के तत्कालीन शासकों से है। यह महल क्योंथल राज्य के पूर्व राज्य का हिस्सा रहा और जुब्बल रियासत के तत्कालीन शासकों के अंतर्गत आता था। ऐसा माना जाता है कि यह रानी का निवास स्थान हुआ करता था। कसुम्पटी से आगे स्थित, यह अद्भुत संपत्ति अपने आप में इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। इस खूबसूरत ईमारत को धज्जी दीवार से बनाया गया है। फर्श से लेकर दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों तक, इस इमारत में अधिकतर लकड़ी का काम किया गया है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस महल से पहाड़ों का अद्भुत 360 डिग्री का नज़ारा दिखाई देता था। 1979 में जिला सोलन के कसौली से राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान को यहां स्थानांतरित किया गया था, तब से यह इमारत स्वास्थ्य विभाग के अधीन है। आज, अधिकांश लोग इस ईमारत की भव्यता और इतिहास को भूल चुके हैं। ठुकरा दिए थे पद्मश्री और पद्मविभूषण सम्मान उस्ताद विलायत खान भारत के पहले संगीतकार थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद इंग्लैंड जाकर संगीत पेश किया था । विलायत ख़ाँ ने सितार वादन की अपनी अलग शैली, गायकी शैली, विकसित की थी जिसमें श्रोताओं पर गायन का अहसास होता था। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फ़ख़रूद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफ़ताब-ए-सितार का सम्मान दिया था और ये सम्मान पानेवाले वे एकमात्र सितारवादक थे। उस्ताद विलायत खाँ ने 1964 में पद्मश्री और 1968 में पद्मविभूषण सम्मान ये कहते हुए ठुकरा दिए थे कि भारत सरकार ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान का समुचित सम्मान नहीं किया।
ब्रिटिश हुकूमत के दौरान शिमला हिंदुस्तान की समर कैपिटल थी और कई महत्वपूर्ण महकमे इसी शहर से चलते थे। शिमला की पुरानी इमारतें आज भी इसकी गवाह है। ऐसी ही एक इमारत में आज इंडियन आर्मी ट्रेंनिंग कमांड है, और ये वही इमारत है, जहां कभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का मुख्यालय था। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जीत की लिए इसी इमारत में रणनीतियां तैयार की जाती थी, यहाँ की दीवारें आज भी इसकी गवाह है। दरअसल साल 1864 से साल 1939 तक भारतीय सेना का मुख्यालय शिमला में था। तब कमांडर-इन-चीफ के अतिरिक्त सेना और सिविल प्रतिष्ठानों के दफ्तरों को स्थापित करने के लिए यहां ईंट, लोहे और कंक्रीट से यह मज़बूत ढांचे को खड़ा किया था। यह निर्माण रिचर्डसन और कुडास फर्म ने सितंबर 1882 से मार्च 1885 के बीच किया और इसे लंदन के पीबॉडी भवनों के डिज़ाइन पर ही बनाया गया था। सरकारी प्रेस और मेसोनिक हॉल भी यहीं बनाए गए थे। उस वक्त कमांडर-इन-चीफ का दफ्तर सबसे ऊपरी ब्लॉक में था और प्रथम और द्वितिय विश्व युद्ध के दौरान सभी ऑपरेशनों की योजना इन्हीं दफ्तरों में बनती थी। सात ऑपरेशनल कमानों में से एक है शिमला आरट्रैक आजादी के बाद भारतीय सेना की पश्चिमी कमान बनाई गई और साल 1954 से साल 1985 तक इन्हीं भवनों में इसका मुख्यालय रहा। साल 1965 और साल 1971 में भारत-पाक युद्धों की योजना भी यहीं बनी। फिर 1985 में जब पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। तदोपरांत 1991 में महु में स्थापित हुए आर्मी ट्रेनिंग कमांड साल 1993 में शिमला के लिए ट्रांसफर कर दी गई और तब से यह मुख्यालय इन्हीं भवनों में स्थापित ह। सेना के सात ऑपरेशनल कमानों में से एक, आरट्रैक भारतीय सेना के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी निभा रहा है।
शर्तों के साथ कोटि के राजा ने लीज़ पर दिया था 'दि रिट्रीट' हिमाचल की राजधानी शिमला के मशोबरा में स्थित राष्ट्रपति निवास ‘दि रिट्रीट’ को पूर्व में प्रेजिडेंशियल रिट्रीट कहा जाता था। वर्ष 1850 में इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण हुआ था। इसे लॉर्ड विलियम ने कोटि के राजा से लीज़ पर लिया था, लेकिन राजा ने लीज़ पर देने से पहले कुछ दिलचस्प शर्तें रखी थीं। इन शर्तों में कहा गया था कि शिमला और मशोबरा गांव से दो सड़कें आम जनता के लिए खुली रहेंगी, यहाँ कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और किसी भी मवेशी को मारा नहीं जाएगा। लीज़ पर देने के कुछ साल बाद, 1886 में कोटि के राजा ने यह भवन वापस ले लिया। लेकिन 1895 में तत्कालीन वायसराय ने इस भवन पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। उस समय वायसराय यहां सप्ताहांत और छुट्टियां बिताने आया करते थे। देश की आज़ादी के बाद इस भवन को राष्ट्रपति निवास के रूप में तब्दील कर दिया गया। देवदार के पेड़ों से घिरे इस आलीशान भवन का समृद्ध इतिहास रहा है। निर्माण के लगभग 175 साल बाद भी इस इमारत की चमक लोगों को आकर्षित करती है। राष्ट्रपति भवन में पहले आम लोगों की आवाजाही पर रोक थी, लेकिन 23 अप्रैल 2023 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। भारतीय नागरिक ₹50 और विदेशी नागरिक ₹250 शुल्क देकर राष्ट्रपति भवन का दीदार कर सकते हैं। यहां लोग राष्ट्रपति के जीवन से जुड़ी स्मृतियाँ, डाइनिंग हॉल, बगीचे, ट्यूलिप गार्डन, सजावटी फूल और अन्य कलाकृतियाँ देख सकते हैं।
लोक रंगमंच हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग है। नृत्य, गायन, संगीत की तरह ही, लोकनाट्य के बगैर भी यहाँ मेले - त्यौहार पूर्ण नहीं होते। अलबत्ता बदलते वक्त ने लोकनाट्य की कई विधाओं को कुछ हद तक अप्रचलित किया हो, पर अब भी लोकनाट्य हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। ये लोकनाट्य इतिहास, धर्म, संस्कृति और किंवदंतियों पर आधारित हैं। ठोडा ठोडा हिमाचल प्रदेश की युद्ध परंपरा से जुड़ा लोकनाट्य है, जो जिला शिमला, सिरमौर तथा सोलन में नाटी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ये महाभारत युद्ध की याद ताजा करता है। यह खेल बैशाखी के दिन से लेकर श्रावण के अंत तक ग्राम देवता मंदिर के सामने खुले आंगन या समतल खुले स्थानों पर खेला जाता है। स्थानीय जनुश्रुति के अनुसार कौरवों की संख्या सौ नहीं साठ थी, इसलिए उन साठ की संतान को शाठा कहते है। पाण्डव पांच ही थे उनके वंशज पाठा या पाशा कहलाते है। शाठी लोग पाशी को खेल के लिये बुलाते थे तो दोनों दल अपने आराध्य देवता की पूजा के पश्चात् फारसो, डंडों, गडासों, धनुष–बाण और तलवारों से आपस में ठोडा खेल खेलते है। बांठडा लोकनाट्य बांठडा का प्रचलन मण्डी तथा उससे लगते क्षेत्रों में है। एक दौर में बांठडा राजमहलों का लोकनाट्य था । शिव, गणपति और सरस्वती की पूजा के साथ बांठडा का आरम्भ होता है, फिर स्थानीय देवता की अराधना की जाती है। इसमें रांझू–फूलमू, कुंजू–चंचलों, राजा–गद्दन आदि की लोक कथाएं भी की जाती है । इसके अतिरिक्त बांठडे में लोकनाट्य जैसे– राजा हरिश्चंद्र, शिव-पार्वती, पूर्ण भक्त इत्यादि भी प्रस्तुत किए जाते है। हरण हरण नृत्य चम्बा में हरणातर, किन्नौर में हौरिंगफों और कुल्लू में होरण के नाम से जाना जाता है। इस लोक नाट्य के दो पक्ष होते है, एक नृत्य पक्ष और दूसरा स्वांग पक्ष। नृत्य में तीन पात्र, हरण, बूढ़ी और कान्ह अपने पारंपरिक वेश भूषा में हिरण का रूप तैयार करके खलिहान में नृत्य करते है। नृत्य के उपरांत स्वागीं पक्ष प्रवेश करता है जो कि स्वागीं मुंह पर कई रंग और कई प्रकार के मुखौटे पहने होते हैं। ढोल नगाडे आदि धुनों पर सामाजिक परिवेश में घटित घटनाओं, समस्याओं सामाजिक बुराईयों तथा हास्य व्यंग्यों को जोड़ कर लोगों का मनोरंजन करते है। भगत भगत लोक नाट्य का प्रचलन विशेषकर कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर जनपद में है। भगत के निर्देशक को गुरू जी और अन्य कलाकारों को भगतिए कहा जाता है। इस नाटक में स्त्री का अभिनय भी पुरूष ही करता है। भगत में गुरूजी पहले अलाव के इर्द -गिर्द घूमता हुआ अग्नि देवता का पूजन करता है और श्री कृष्ण के लीला-गान इसका मुख्य विषय होते है। भगत में एक पात्र को कृष्ण बनाया जाता है और चार- पांच सखियां बनायी जाती हैं। फिर इस में हंसी मजाक इत्यादि करके लोगों का मनोरंजन किया जाता है । करियाला करियाला हिमाचल प्रदेश का बहुचर्चित लोक नाट्य है जिसका मंचन सिरमौर, शिमला और सोलन जिले में वर्ष भर किया जाता है। किसी मंच पर नहीं , अपितु त्यौहारों, मेलों, अनुष्ठानों, देवताओं के जागरण पर खुले प्रांगण में करियाला होता है। इस में खुले स्थान पर लकड़ियां इक्कठा करके अलाव जलाकर उसके चारों ओर लोग खडे हाते है, जिसे अखाड़ा भी कहते है। एक किनारे पर ढोलक, खंजरी, दमामटा, चिमटा, बांसुरी और नगाडा आदि वाद्ययंत्र लिए बंजतरी बैठ जाते है। चंदरौली करियाला का प्रमुख पात्र यह स्त्री वेशभूषा पहने पुरूष ही होती है। बजंतरियों द्वारा बधाई ताल बजते ही चंदरौली प्रवेश करती है। चंदरौली अपना अलाव का पूरा फेरा पूरा करने के उपरांत चारों दिशाओं से तीन-चार साधु अलख जगाते हुए मंच पर आतें है। इन साधुओं द्वारा समाज के ज्वलंत मुद्दों अंधविश्वासों, ज्ञानी-ध्यानी, मुनि- तपस्वी तथा तंत्र-मंत्र की बातों से लोगों का हास्य व्यंग्यों से मनोरंजन करते है । बरलाज लोक नाट्य बरलाज मूल रूप से गीति काव्य नाट्य है। हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में कार्तिक की अमावस्या बूढ़ी दिवाली के नाम से मनाई जाती है। बरलाज लोकनाट्य सोलन व सिरमौर में रामायण के प्रसंगों सहित प्रस्तुत किया जाता है। दीपावली के आस-पास देवताओं के मन्दिरों में मेले लगते हैं। रात को मन्दिर के सामने खुले आंगन/ मैदान में लकड़ियों के ढेर लगाकर गीट्ठा (घियाना) जलाया जाता है । सबसे पहले खेल के आरम्भ होते ही गीठे के चारो ओर देवता के वाद्य यंत्रों की धुनों में परिक्रमा की जाती है। देवता के चेला को खेल आती है और लोगों को चावल के दाने बांटता है। तब रामायण के अनेक प्रसंग प्रस्तुत किये जाते हैं । हनुमान से सम्बन्धित दृश्य को हणु, लक्ष्मण, सीता के प्रसंग दो-तीन कलाकार स्थानीय भाषा में प्रसंग गाकर प्रस्तुत करते हैं ।
जब भी राष्ट्र पर संकट आया वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के शौर्यवीरों ने नया इतिहास लिख दिया। ये बेहद गौरव का संदर्भ है कि देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान 'परमवीर चक्र, अब तक महज 21 वीर सपूतों को प्राप्त हुआ है, और इनमें हिमाचल के चार योद्धा शामिल है। वीरता और देश भक्ति का जज्बा यहाँ के हवा -पानी में घुला है और हर साल हजारों हिमाचल युवा सेना में भर्ती होते है। हिमाचल के हर जिले, हर हिस्से, हर गांव में युवाओं में सेना भर्ती को लेकर एक सा जूनून और जोश दिखता है। वीरों का ऐसा ही एक गांव जिला सिरमौर की शिलाई तहसील में स्थित जास्वी गांव है , जो वीरता और जज्बे की एक अद्भुत मिसाल पेश करता है। इस छोटे से गांव में 48 घर हैं और करीब 800 की आबादी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां के हर घर से कोई न कोई भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहा है, या दे चूका है। जास्वी गांव न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अनूठी परंपरा और वीरता के कारण भी चर्चा में रहता है। जास्वी गांव ने हर घर से एक फौजी की परंपरा को जीवित रखा है और इसे गर्व के साथ आगे बढ़ाया है। जास्वी गांव में वर्तमान में 30 जवान भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां के लोग मानते हैं कि हर घर से एक जवान सेना में होना चाहिए। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इनका एक नैतिक कर्तव्य बन चुका है। जब भी सेना को आवश्यकता होती है, इस गांव के युवा सीमाओं पर तैनात होने के लिए तैयार रहते हैं। गांव के लोग बताते है कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे गांव से हर घर में एक जवान है। यह परंपरा हम पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आ रहे हैं। जब भी मातृभूमि को आवश्यकता होती है, हम सीमाओं पर डटे रहते हैं। जास्वी गांव के अधिकांश लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यहां के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होना एक सपना बन चुका है। यहां के लोग मानते हैं कि देश की सेवा से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता और यही कारण है कि यहां के युवा सेना में भर्ती होने के लिए कठिन मेहनत करते हैं। इस गांव की प्रधान चमेली जस्टा बताती हैं कि- "हमारे गांव से अब तक कई लोग सेना में सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में 30 युवा सेना में हैं, और हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारा गांव देश की सेवा में अपनी भागीदारी निभा रहा है। यहां के लोगों में यह भावना समाई हुई है कि हर घर से एक जवान सेना में तैनात हो, ताकि हमारे देश की सुरक्षा मजबूत हो।" जास्वी गांव के जस्टा परिवार के बारे में कहा जाता है कि इस परिवार के अधिकांश सदस्य सेना में हैं। अत्तर जस्टा बताते हैं, “हमारे परिवार में पांच भाई सेना में हैं, जिनमें से तीन सगे भाई (प्रकाश, विक्रम और मनोज) हैं, और दो चचेरे भाई हैं। मैं खुद भी सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश भर्ती नहीं हो सका।” उनका कहना है कि “हमारे लिए सेना में भर्ती होना सबसे बड़ा सम्मान है और यह सम्मान हम अपने परिवार और गांव के लिए हर हाल में निभाना चाहते हैं। जास्वी गांव की यह वीरता सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गांव अपने बलिदान, निष्ठा, और देशभक्ति की कहानी बयां करता है।
हिमाचल में कई दिलचस्प लोककथाएं प्रचलित है, जो जीवन के हर पहलु को छूती है। काफल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध फल है, जो अपनी मीठी और खट्टी-मीठी स्वाद के लिए जाना जाता है। काफल से जुडी एक रोचक लोककथा बेहद लोकप्रिय हैं। एक गांव में एक निर्धन महिला अपनी 6-7 साल की बेटी के साथ रहती थी। किसी तरह वो दोनों अपना गुजर बसर करते। एक बार माँ सुबह सवेरे घास के लिए गयी और घास के साथ काफल फल तोड़ के लायी। बेटी ने काफल देखे तो बड़ी खुश हुई। माँ ने कहा कि मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, जब लौटूंगी तब काफल खाएंगे। इसके बाद उसने काफल एक टोकरी में रख दिए। बेटी दिन भर काफल खाने का इंतज़ार करती रही। बार बार टोकरी के ऊपर रखे कपड़े को उठा कर देखती और काफल के खट्टे-मीठे रसीले स्वाद की कल्पना करती, लेकिन उस आज्ञाकारी बच्ची ने एक भी काफल उठा कर नहीं चखा। जब माँ लौटकर आई तो बच्ची दौड़ के माँ के पास गई, और केहनी लगी 'माँ अब काफल खाएं ?' पर जब महिला ने काफल की टोकरी निकाली, तो उसे फल कम लगे। दरअसल काफल सुख चुके थे और महिला इसे समझ नहीं पाई। बगैर सोचे समझे उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में बच्ची के सर पे जोर का प्रहार कर दिया। बच्ची उस अप्रत्याशित वार से तड़प के नीचे गिर गयी और उसके प्राण पखेरू उड़ गए। ”मैंने नहीं चखे माँ” कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। महिला का क्षणिक आवेग उतरा तो उसके होश उड़ गए। अपनी बच्ची को गोद में ले कर वह प्रलाप करने लगी। उस दुखियारी का एक मात्र सहारा उसने अपने ही हाथ से खत्म कर दिया था , और वो भी तुच्छ काफल की खातिर। आखिर उसी बेटी के लिये तो वो काफल लाई थी, तो क्या हुआ था जो उसने थोड़े खा लिए थे। विलाप करते हुए उसने उठा कर काफल की टोकरी बाहर फेंक दी। रात भर वह रोती बिलखती रही। दरअसल जेठ की गर्मी से काफल कुम्हला कर थोड़े कम हो गए थे, पर रात भर बाहर ठंडी व नर्म हवा में रहने से वे सुबह फिर से खिल गए और टोकरी भर गई। अब माँ की समझ में आया थी कि उसकी बेटी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। रोते बिलखते हुए उसने भी प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि वे दोनों मां - बेटी मर के पक्षी बन गए। कहा जाता है कि वह घुघुती पक्षी बनकर लौट आये, जो आज भी अपनी आवाज से काफल की लोककथा सुनाते है। जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है ”काफल पाको ,मैं नी चाखो ” (काफल पके हैं, पर मैंने नहीं चखे हैं) और तभी दूसरा पक्षी चीत्कार कर उठता है “पुर पुतई पूरपूर ” (पूरे हैं बेटी पूरे हैं) ! कुदरत का फल : काफल काफल हिमाचल और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ‘मेरिका एस्कूलेंटा’, और हिमाचल -उत्तराखंड में इसे कुदरत का फल माना जाता है। दरअसल यह फल जंगलों में स्वाभाविक रूप से उगता है और विभिन्न जानवरों और पक्षियों द्वारा फैलाया जाता है। आमतौर पर बान और बुरास के जंगलों में पाया जाने वाला काफल खासकर सिरमौर, मंडी, कुल्लू, शिमला, चम्बा जैसे क्षेत्रों में बहुतायत से उगता है। काफल न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। आयुर्वेद में काफल को एक महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है।
कुल्लू में भांग के रेशों से बनने वाली पारंपरिक चप्पल, जिन्हें आम भाषा में "पूलें" कहा जाता है, यहाँ की संस्कृति का हिस्सा रही हैं। यहां के ग्रामीण परिवेश में पूलें (चप्पलें) सदियों से शामिल रही हैं। हालांकि, समय के साथ इनका प्रचलन कम हुआ, पर बीते कुछ सालों में इन्हें व्यावसायिक पहचान मिलने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे कुल्लू की टोपी, शॉल, मफलर और जुराबों को मिलती रही है। ये पारंपरिक चप्पल ग्रामीण लोगों को सर्दियों में गरम रखती हैं। ग्रामीण इलाकों में पुराने समय से इनका इस्तेमाल आम है। कुल्लू की पूलें आरामदेह होने के साथ-साथ पवित्र भी हैं। इन्हें भांग के रेशे के साथ-साथ जड़ी-बूटियों से तैयार किया जाता है। भांग के पत्ते के तने के साथ ही ब्यूल के रेशों का भी इसे बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी ग्रामीण इलाकों में पुराने समय से ही भांग के रेशों का व्यावसायिक इस्तेमाल होता आ रहा है। ये पूलें काफ़ी मजबूत होती हैं। शुरुआती दौर में साधारण दिखने वाली पूलें बनाई जाती थीं, जिन्हें सिर्फ भांग के रेशे से बनाया जाता था। समय के साथ इनके डिज़ाइन में रंगीन धागों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इन पूलों का तला भांग के पौधे के रेशों से बनता है, जबकि ऊपर का हिस्सा रंगीन धागों से बनाया जाता है। इसके रंगीन चमकीले धागों से हिमाचली डिज़ाइन शैली की झलक साफ़ दिखती है। एक पूल का जोड़ा बनाने में तीन से चार दिन का समय लगता है। शुभ कार्यों में किया जाता है इस्तेमाल आज भी शुभ कार्यों के वक्त ये पूलें इस्तेमाल में लाई जाती हैं। दरअसल, इन्हें पहनकर देव-स्थल के भीतर जाने में कोई पाबंदी नहीं होती। मंदिरों में जहां देवी-देवताओं के आसपास जूते-चप्पल ले जाना निषेध होता है, वहां साफ़ नई पूलें पहनी जाती हैं। कुल्लू में धाम के वक्त वोटी (रसोइया) द्वारा भी पूलें पहनकर खाना बनाया जाता है। प्रधानमंत्री भी मुरीद कुल्लू की इस पारंपरिक चप्पल के मुरीद ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। इनकी ख़ासियत को जानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल्लू की पूलों को काशी विश्वनाथ के पुजारियों, सेवकों और सुरक्षाकर्मियों के लिए खड़ाऊ का बेहतरीन विकल्प माना और इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। इसके बाद से ही इनकी मांग में तेज़ी भी आई।
हिमाचल की वादियों में छिपी प्रेम कहानियां केवल लोकगीतों में ही नहीं, बल्कि पत्थरों और लकड़ियों में भी दर्ज हैं। जैसे ताजमहल मुमताज और शाहजहां के प्रेम की अमर निशानी है, वैसी ही एक प्रेमगाथा कुल्लू की बंजार घाटी में आज भी जीवित है चैहणी कोठी के रूप में। बंजार से 5 किलोमीटर और शृंगा ऋषि मंदिर बग्गी से महज एक किलोमीटर दूर स्थित यह कोठी न सिर्फ स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है, बल्कि एक सच्चे प्रेम की जीवंत मिसाल भी। कहते हैं इस क्षेत्र के ठाकुर ढाढिया का अपनी पत्नी चैहणी से अपार प्रेम था। जब चैहणी का देहांत हुआ, तो उस प्रेमी ने अपने टूटे दिल की याद में यह आलीशान कोठी बनवाई। आज यह कोठी न सिर्फ स्थापत्य प्रेमियों को लुभाती है, बल्कि प्रेम की उस निशानी को भी हमेशा के लिए संजोए हुए है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस कोठी की ऊंचाई कभी 15 मंजिलों तक जाती थी। लेकिन 1905 के विनाशकारी भूकंप ने इसकी पांच मंजिलें गिरा दीं। फिर भी, आज भी 10 मंजिलें शान से खड़ी हैं। पहले पांच मंजिलें पत्थर की हैं और ऊपर की चिनाई ‘कुल्लुई काठकुणी’ शैली में लकड़ी और पत्थर से की गई है। कोठी के पास स्थित है एक और अद्भुत संरचना है शृंगा ऋषि का भंडारगृह, जो कोट शैली में बना पांच मंजिला ढांचा है। इसमें देवता का अनाज, बर्तन और ढाढिया ठाकुर की तलवारें आज भी रखी गई हैं। इस कोठी में ठाकुर के वंशज आज भी रहते हैं, और शृंगा ऋषि का मोहरा अब भी धार्मिक अनुष्ठानों में गांव-गांव ले जाया जाता है। वहीं, इस कोठी से महज 20 फुट दूर स्थित है भगवान मुरली मनोहर का प्राचीन मंदिर, जिसका निर्माण मंडी के राजा मंगल सेन ने करवाया था। मंदिर की मूर्ति मंगलौर से मंगवाई गई थी, और आज भी यह मंदिर होली व जन्माष्टमी पर उल्लास का केंद्र होता है। यहां के लोग कहते है कि चैहणी कोठी केवल एक इमारत नहीं, बल्कि प्रेम, विरासत, और संस्कृति का त्रिवेणी संगम है। इसकी लकड़ी की शहतीरें, झरोखे और पत्थरों में छुपा इतिहास आज भी सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है।
कांगड़ा चाय अपनी गुणवर्ता के लिए पूरी दुनिया में विशिष्ठ पहचान रखती है। ब्रिटिश राज के दौरान कांगड़ा में चाय उगाने की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले साल 1848 में अंग्रेजों ने इसे लेकर सर्वे किया था। बोटोनिकल गार्डन्स ऑफ़ नार्थ वेस्ट प्रोविंस के सुपरिंटेंडेंट डॉ जेम्ससन ने ये सर्वे करवाए थे। 1848 में डॉ जेम्ससन पेशावर से कांगड़ा आये और उन्हें धौलाधार रेंज के कई क्षेत्र चाय उगने के लिए उपयुक्त लगे। इसके बाद 1852 में पालमपुर के होलटा में चाय उगाने की शुरुआत हुई। 1857 में पालमपुर में पहला टी एस्टेट लगा जिसका नाम 'वाह टी एस्टेट' है। ये वाह के नवाब द्वारा लगया गया था और वाह क्षेत्र अब पाकिस्तान में आता है। 'वाह टी स्टेट' आज भी मौजूद है। इसके आबाद धीरे धीरे चाय के बागान बढ़ते गए और आज कांगड़ा चाय वैश्विक पटल पर अपनी अलग पहचान बनाये हुए है।
शिव नगरी बैजनाथ में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। यहां ऐसी धारणा भी है कि किसी ने रावण जलाया या दशहरा मनाया तो उसे भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि बैजनाथ मंदिर में वही शिवलिंग है, जिसे लंकापति रावण हिमालय में भगवान शिव की तपस्या करने के बाद लंका ले जा रहा था, लेकिन एक शर्त पूरी न कर पाने के कारण यह यही स्थापित हो गया था। यहां सालों से दशहरा पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता था। दरअसल 1965 में बैजनाथ भजन मंडली का गठन हुआ। इसमें शामिल कुछ बुजुर्ग व युवाओं ने उस समय मंदिर के ठीक सामने मैदान मे दशहरा मनाने की प्रथा शुरू की लेकिन भजन मंडली के अध्यक्ष की उसके कुछ समय बाद मौत हो गई। साथ ही इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ लोगों को मौत व भारी हानि का सामना करना पड़ा। इसका बाद 1969 में यहां दशहरा मनाना ही बंद कर दिया गया। इसके पीछे कुछ लोगों का तर्क था कि लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था और कोई भी देव अपने भक्त को इस तरह से जलता नहीं देख सकता। न यहां दशहरा उससे पहले मनाया जाता था और न ही उक्त चार सालों के बाद कभी मनाया गया है।
दुनिया में ऐसा शायद ही कोई बाजार होगा, जहां सुनार यानी ज्वेलर्स की दुकान न हो। किन्तु हिमाचल प्रदेश में एक शहर ऐसा भी है, जहां एक भी सुनार की दुकान नहीं है। जिला कांगड़ा के बैजनाथ में सुनार की एक भी दुकान नहीं है। जबकि इस शहर के महज एक किलोमीटर या कहें साथ में बसे दूसरे कस्बे पपरोला में सुनार की दर्जनों छोटी बड़ी दुकानें हैं। ऐसा माना जाता है कि बैजनाथ में जिस ने भी कभी सुनार की दुकान खोली या तो उसे काफी घाटा हुआ या फिर आग ने दुकान को जलाकर राख कर दिया। 70 के दशक तक भी यहां कोई सुनार की दुकान नहीं थी। कहा जाता था कि बैजनाथ में न दशहरा हो सकता है और नही यहां सुनार की दुकान खुल सकती है। बावजूद इसके वर्ष 1975 के आसपास यहां एक सुनार ने दुकान शुरू की। दुकान शुरू किए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि दुकान आग की भेंट चढ़ गई। इसके बाद कुछ दुकानें और शुरू हुई थी, लेकिन वे दुकानें भी घाटे में जाकर बंद हो गई। इसके बाद फिर किसी ने यहां सोने चांदी का कारोबार करने की हिम्मत नहीं की। इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन कहीं न कहीं इसका संबंध यहां मौजूद शिव मंदिर से जोड़ा जाता है।
2 मार्च 2017 को प्रदेश की वीरभद्र सरकार ने धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बनाने का फैसला लिया। पर धर्मशाला को राजधानी का दर्जा देने की कवायद नई नहीं थी। दरअसल इसकी शुरुआत करीब डेढ़ सौ साल पहले हो गई थी। ब्रिटिश शासनकाल में 1863 में वाइसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन धर्मशाला आए थे और उन्होंने लंदन में ब्रिटिश सरकार को यह प्रस्ताव भेजा कि धर्मशाला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया जाए। इस बीच 20 नवंबर 1863 को धर्मशला में ही लॉर्ड एल्गिन की मौत हो गई। उन्हें मैक्लॉडगंज के सेंट जोन्स चर्च में दफनाया गया था। इसके साथ ही धर्मशला को दूसरी राजधानी बनाने की उनकी मंशा भी दफ़न होकर रह गई। इस दौरान अंग्रेजों को शिमला भा गया और 1864 में शिमला गीष्मकालीन राजधानी बनी। इसके करीब 154 साल बाद 2017 में धर्मशाला को देश की तो नहीं लेकिन हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का दर्जा मिला। वाइसराय लॉर्ड एल्गिन चाहते थे धर्मशाला को हिंदुस्तान की राजधानी बनाना 2 मार्च 2017 को प्रदेश की वीरभद्र सरकार ने धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बनाने का फैसला लिया। पर धर्मशाला को राजधानी का दर्जा देने की कवायद नई नहीं थी। दरअसल इसकी शुरुआत करीब डेढ़ सौ साल पहले हो गई थी। ब्रिटिश शासनकाल में 1863 में वाइसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन धर्मशाला आए थे और उन्होंने लंदन में ब्रिटिश सरकार को यह प्रस्ताव भेजा कि धर्मशाला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया जाए। इस बीच 20 नवंबर 1863 को धर्मशला में ही लॉर्ड एल्गिन की मौत हो गई। उन्हें मैक्लॉडगंज के सेंट जोन्स चर्च में दफनाया गया था। इसके साथ ही धर्मशला को दूसरी राजधानी बनाने की उनकी मंशा भी दफ़न होकर रह गई। इस दौरान अंग्रेजों को शिमला भा गया और 1864 में शिमला गीष्मकालीन राजधानी बनी। इसके करीब 154 साल बाद 2017 में धर्मशाला को देश की तो नहीं लेकिन हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का दर्जा मिला।
हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में परंपरागत घराट का चलन सदियों से चला आ रहा हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग गेहूं की घराट से पिसाई करते हैं। इनसे जो आटा निकलता है उसकी तुलना चक्की के आटे से नहीं की जा सकती। इस आटे को चक्की के आटे से ज्यादा बेहतर माना जाता है। यही वजह है कि आज भी ग्रामीण लोग घराट के आटे का ही इस्तेमाल करते हैं, हालांकि अब इसका चलन काफी कम होता जा रहा है। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में वो दौर भी था जब घराट ग्रामीण लोगों के लिए आर्थिकी का मुख्य साधन बना। लोग अपने खेतों में पारंपरिक अनाजों और गेंहू, कोदा का उत्पादन कर उसे पानी से चलने वाले घराटों में पीसकर आटा तैयार करते थे। इन घराटों में पिसा हुआ आटा कई महीनों तक तरोताजा रहता था। खास बात यह थी कि आटे की पौष्टिकता बनी रहती थी और मिलावट के नाम पर कुछ नहीं होता था। शायद यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग स्वस्थ रहते थे और सेहत का राज भी हुआ करता था। इन घराटों में लोग कोदा, गेहूं, मक्का, चेस्टन जैसे स्थानीय अनाज पीसा करते थे। घराट संचालक घराटों में गेहूं पीसने के साथ ही बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी कार्य करते थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इससे रोजगार भी सृजित होते थे। किन्तु जब से अत्याधुनिक मशीनों का निर्माण हुआ, तब से उन मशीनों पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में अब कम ही घराट नजर आते हैं। अब घराट विलुप्त होने की कगार पर है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हिमाचल की राजधानी शिमला से गहरा नाता रहा है। उनकी विचारधारा और रणनीतियों को आकार देने वाले विभिन्न क्षेत्रों में से एक शिमला भी है l हिमालय की ऊँची चोटियां भी उनके गहन राजनीतिक दर्शन और रणनीतिक चिंतन की साक्षी रही। बेशक आजादी के बाद महात्मा गांधी शिमला नहीं आ पाए, मगर आजादी से पहले शिमला बापू की कर्म स्थली रही। इतिहास के गर्भ में छिपे कई महत्वपूर्ण फैसले राजधानी शिमला में ही हुए, यहाँ उनकी अनेक स्मृतियां भी मौजूद हैं। राष्ट्रपिता की अधिकांश शिमला यात्राएं ब्रिटिश सत्ता के साथ चर्चा से जुड़ी हुआ करती थी। महात्मा गांधी की पहली शिमला यात्रा 11 मई 1921 में हुई। तब बापू मौलाना मुहम्मद अली, शौकत अली, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपतराय के साथ तत्कालीन लॉर्ड रीडिंग से मिलने शिमला आए थे। उस यात्रा में वे शिमला के चक्कर में शांति कुटीर में ठहरे थे। तब ये मकान होशियारपुर के साधु आश्रम की संपत्ति थी। 13 मई को गांधी जी वायसराय लॉर्ड रीडिंग से मिले l दूसरे दिन महात्मा गांधी ने आर्य समाज लोअर बाजार शिमला के हॉल में महिलाओं को संबोधित किया, 15 मई को उन्होंने 15000 से अधिक के जन समूह को ईद के मौके पर संबोधित किया l शिमला के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र से भी लोग गांधी के दर्शन के लिए आए थे l गांधी जी के शिमला आगमन से ही इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का ध्यान राष्ट्रीय विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ था l इसके बाद वे 1931 में वायसराय लार्ड वेलिंग्टन से मिलने भी आए थे। सितंबर 1939 में वे दो बार और 1940 में एक बार शिमला आए। महात्मा गांधी अपनी अंतिम शिमला यात्रा के दौरान 1946 में आए। ये यात्रा दो हफ्ते की थी। इस दौरान वे समरहिल में चैडविक इमारत में ठहरे। शिमला से पहले डगशाई आए थे बापू शिमला से पहले महात्मा गांधी सोलन की डगशाई जेल 1920 में आए थे। दरअसल, प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने बड़ी संख्या में आयरिश सैनिकों को बंदी बनाया था। इनमें से कइयों को हिमाचल लाकर डगशाई जेल में बंद करके कठोर यातनाएं दी गई। आयरिश सैनिकों ने जेल की प्रताड़ना सहते हुए यहां अनशन भी किया था। यह बात जब जेल से बाहर निकली तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी उन्हीं सैनिकों से मिलने डगशाई आए। इस दौरान वह 2 दिन तक इसी जेल में रुके। बताते हैं कि गांधी जी, आयरिश नेता इयामन डे वेलेरा के दोस्त और प्रशंसक भी थे। यही कारण था कि हिंदुस्तान की जेल में बंद होकर भी अपनी आजादी की जंग लड़ रहे आयरिश सैनिकों से मिलने बापू डगशाई पहुंचे। उस समय बापू को जिस कोठरी में ठहराया गया था, उसके बाहर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। इसी जेल का आखिरी कैदी महात्मा गांधी का हत्यारा नाथू राम गोडसे था। शिमला में हुआ महात्मा गांधी की हत्या का ट्रायल महात्मा गांधी की हत्या का ट्रायल शिमला के मिंटो कोर्ट में चला। तत्कालीन समय में मिंटो कोर्ट पीटरहॉफ के अधीन था, जहां अब हिमाचल सरकार का राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ चल रहा है। इसी मिंटो कोर्ट में नाथू राम गोडसे को बतौर आरोपी पेश किया गया। 21 जून 1949 को गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद अंबाला जेल में गोडसे को फांसी दी गई। तब पंजाब हाईकोर्ट भी इसी भवन में था, हालांकि अब यह मिंटो कोर्ट भवन जलकर राख हो गया है। इसी के साथ नाथू राम गोडसे से जुड़ा इतिहास भी खत्म हो गया। साल 1968 में मिंटो कोर्ट को दीपक प्रोजेक्ट के सुपुर्द किया गया, तब से यहां इनका कार्यालय चल रहा है। शिमला में चलने वाले मानव रिक्शा से निराश थे महात्मा गांधी आजादी से पहले शिमला में सिर्फ तीन ही गाड़ियां होती थी l ज्यादातर लोग मानव रिक्शा से ही सफर किया करते थे। महात्मा गांधी मानव रिक्शा के भी खिलाफ थे। इस रिक्शा को चलाने में पांच लोगों की जरूरत पड़ती थी। चार लोग रिक्शा को खींचते थे, जबकि एक आदमी रिक्शा के पीछे दौड़ा करता था। जब कोई एक व्यक्ति थक जाता, तो दौड़ रहा व्यक्ति उसकी जगह ले लेता था। महात्मा गांधी को जब स्वयं मानव रिक्शा से सफर करना पड़ा तो, वे बेहद निराश हुए। उन्होंने रिक्शा खींच रहे लोगों से पूछा कि क्या तुम पशु हो? तब रिक्शा खींच रहे एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि हम पशु तो नहीं, लेकिन हमारे साथ पेट जुड़ा है। इसके लिए हमें यह काम करना पड़ता है, हालांकि धीरे-धीरे समय बदला और समय के साथ मानव रिक्शा का अस्तित्व ही खत्म हो गया।
आर्थिक सम्पन्नता के बावजूद समुदाय के कई लोग करते है भेड़े चराने का काम हिमाचल की सड़कों पर कभी कभार भेड़-बकरियों को हांकते कुछ गडरिये दिख जाया करते है। ये लुभावना कारवां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। न सिर्फ पर्यटक बल्कि ये दृश्य उन दार्शनिक विभूतियों को भी अपनी तरफ खींचता है जो जीवन जीने के मुख़्तलिफ़ तौर तरीकों में दिलचस्पी रखते है। ये भोलेपन और सादगी की मूरत कहे जाने वाले हिमाचल के गद्दी समुदाय का कारवां होता है, जो अपनी इसी अनूठी जीवन शैली के लिए जाना जाता है। गद्दी समुदाय की कहानी हिमाचल के पहाड़ों के बीच बुनी गई उन कहानियों में से एक है जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुना और सुनाया जाता रहा है। हिमाचल के पहाड़ों में यूँ तो कई समुदाय बस्ते है मगर अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, रहन-सहन, रीति-रिवाज और पहनावे के कारण गद्दी जनजाति अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। गद्दी समुदाय उन समुदायों में से एक है जो आज भी अपनी संस्कृति और विरासत को संजोए रखने में कामयाब रहा है। गद्दी जनजाति के लोग आज प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, इंजीनियर, डॉक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपरा को नहीं छोड़ा है। वहीँ अब भी इस समुदाय के कई लोग भेड़े चराने का ही काम करते है। आइए इस समुदाय के बारे में थोड़ा और जानते है। गद्दी जनजाति भारत की सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजातियों में से एक है। पशुपालन करने वाले ये लोग वर्तमान में धौलाधर श्रेणी के निचले भागों, खासकर हिमाचल प्रदेश के चम्बा और कांगड़ा ज़िलों में बसे हुए हैं। शुरू में वे ऊंचे पर्वतीय भागों में बसे रहे, मगर बाद में धीरे-धीरे धौलाधार की निचली धारों, घाटियों और समतल हिस्सों में भी उन्होंने ठिकाने बनाए। गद्दी आज पालमपुर और धर्मशाला समेत कई कस्बों में भी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। चंबा जिला में लगभग चार लाख और कांगड़ा घाटी में लगभग तीन लाख गद्दी रहते हैं। गद्दी जनजाति का उद्गम कहां से हुआ, इसके लिए अलग-अलग कथाएं निकल कर आती हैं। जानकारों के अनुसार वर्षों पहले ये लोग अफगानिस्तान से लाहौर के रास्ते राजस्थान आए थे, परंतु वहां की आबोहवा गर्म होने के कारण ये हिमाचल प्रदेश में आकर बस गए। हालांकि जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में भी इनका बड़ा कुनबा रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की इस जनजाति ने मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त होकर हिमाचल की पहाड़ियों में शरण ली थी। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति पहले मध्य एशिया, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती थी, लेकिन 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों से परेशान होकर गद्दी जनजाति ने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में शरण ली। रंग रूप और कद काठी में गद्दी समुदाय काफी हद तक राजपूत समुदाय से मिलता है। गद्दी समुदाय के लोग स्वयं को गढ़वी शासकों के वंशज मानते हैं। गद्दी जनजाति के लोगों का मानना है कि अपने धर्म, समाज की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में शरण ली है। इस समुदाय के लोग जन्म और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाते हैं तथा अपनी बिरादरी के लोगों के सामाजिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। परंपरागत रीति-रिवाजों से इस समुदाय के लगाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिमाचल से बाहर बसे गद्दी समुदाय के लोगों ने लुधियाना, दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अपने संगठन बना रखे हैं, जिनके माध्यम से वे अपने लोगों और अपनी सभ्यता-संस्कृति से जुड़े रहते हैं। मृत्यु जैसी शोक की घड़ी में समूची गद्दी बिरादरी शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी होती है। मृतक का अंतिम संस्कार सम्पन्न करने वाला परिवार का सदस्य 10 दिनों तक भूमि पर सोता है। इस दौरान उसके सामने चादर बिछाई जाती है। शोक व्यक्त करने आने वाले लोग यथासंभव आर्थिक सहयोग करते हुए चादर पर अपनी क्षमता के अनुसार रुपए-पैसे चढ़ाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ‘बरतन’ कहते हैं। 10 दिन बाद चादर उठाकर एकत्रित राशि शोक संतप्त परिवार को दी जाती है। इस दौरान शोक संतप्त परिवार की बहुएं पारंपरिक परिधान ‘लुआंचड़ी’ पहनती हैं तथा कोई भी जेवर नहीं पहनतीं। अपनी मजबूत सांस्कृतिक पहचान के बावजूद, गद्दी समुदाय को आधुनिक दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक दबाव, बदलते जलवायु पैटर्न और शहरी केंद्रों में पलायन उनके पारंपरिक जीवन शैली के लिए खतरा पैदा करते हैं। गद्दी संस्कृति को संरक्षित करने, स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और शिक्षा और कौशल विकास पहलों के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संगठनों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। संक्षेप में, गद्दी समुदाय एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जहाँ हिमालय की विस्मयकारी सुंदरता के बीच परंपरा आधुनिकता से मिलती है - एक ऐसी दुनिया जो सादगी, सांस्कृतिक समृद्धि और अपने प्राकृतिक परिवेश से गहरे जुड़ाव की विशेषता रखती है। पशुधन के साथ गहरा रिश्ता गद्दी जीवन शैली का मुख्य हिस्सा पशुधन के साथ उनका गहरा रिश्ता है। वे भेड़ और बकरियों को चराने में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं, ये लोग अपने जानवरों के लिए ताज़ा चारागाह खोजने के लिए चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। यह खानाबदोश जीवन शैली न केवल उनकी आजीविका को बनाए रखती है बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को भी दर्शाती है। अपनी भेड़ों से इन्हें काफी उच्च कोटि का ऊन भी मिलता हैं, जिसके माध्यम से यह गर्म कपड़े, शाल, कंबल, जैकेट, ओवरकोट, टोपी बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। गद्दी जनजाति के लोग सर्दियों में अपने पशुओं को लेकर निचले स्थानों पर आ जाते हैं, जबकि गर्मियों में ऊंची पहाड़ियों पर भेड़ बकरियों को लेकर चले जाते हैं। दूल्हे को बारात से पहले बनाया जाता है ‘जोगी’ गद्दी समुदाय में विवाह समारोह के अवसर पर दूल्हे को बारात से पहले ‘जोगी’ बनाया जाता है। इस परंपरा में धोती-कुर्ता के साथ उसे चोला-डोरा पहना कर हाथों में धनुष-बाण दिया जाता है। मान्यता है कि इस दौरान यदि दूल्हा घर की दहलीज से बाहर चला जाए तो ‘जोगी’ बन जाता है। हालांकि इस रस्म को परंपरा के रूप में निभाया जाता है, परन्तु कभी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद पारंपरिक नुआला का आयोजन किया जाता है, जिसमें समुदाय के ब्राह्मण सारी रात भगवान शिव का स्तुतिगान करते हैं। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों से समूचा इलाका गूंज उठता है और समुदाय के लोग पारंपरिक परिधानों में नाचते-गाते हैं। गद्दी जनजाति के लोगों का पहनावा भी अलग है। शुभ अवसरों पर गद्दी महिलाएं पारंपरिक परिधान ‘लुआंचड़ी’, कुर्ता, डोरा पहनती हैं। महिलाओं के गहनों में मुख्यत: और ज्यादातर चांदी से बने चिड़ी, चंद्रहार, संगली, सिंगी, क्लइपड़ू, चक, कंडडू, कंगन और मरीजड़ी होते हैं। ज्यादातर महिलाएं कमर पर चांदी का छल्ला लटकाना नहीं भूलतीं। वहीँ पुरुष सिर पर पगड़ी पहनते हैं। वह डोरा के साथ एक प्रकार का चोला भी पहनते हैं ।
'ओशो’ से हम सभी परिचित हैं l अपने लाखों प्रशंसकों, शिष्यों और अनुयायियों के लिए वो सिर्फ़ ‘ओशो’ थे, भारत और फिर बाद में पूरी दुनिया में उन्हें ‘आचार्य रजनीश’ और ‘भगवान श्री रजनीश’ के नाम से जाना जाता था l भारतीय विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रणेता ओशो को दुनिया से गए साढ़े तीन दशक से अधिक हो चुके हैं लेकिन आज भी उनकी लिखी किताबें बिक रही हैं, उनके वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर आज भी ख़ूब देखे-सुने जाते हैं l ओशो में लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी जगी क्योंकि वो किसी परंपरा, दार्शनिक विचारधारा या धर्म का हिस्सा कभी नहीं रहे l ओशो का हिमाचल से भी गहरा नाता रहा है ल क्या आप जानते है ओशो की बहुचर्चित 'नवसन्यास' या 'नव संन्यास' का जन्म हिमाचल में हुआ था। जीवन जीने के विभिन्न तरीके सीखने वाले ओशो ने नवसन्यास का सिद्धांत हिमाचल में दिया था l 26, सितंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू -मनाली में एक ध्यान शिविर के दौरान ओशो ने “नवसंन्यास” का सूत्रपात किया, जो नये मनुष्य में लिए उनका सबसे सुंदर स्वप्न माना गया l माना जाता है की ओशो ने पुराने संन्यास को, जो अपनी मृत्यु-शैया पर था, पुनर्जन्म दिया था। आधुनिक दुनिया में पुराना संन्यास पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुका था। इस महत्वपूर्ण समय में, ओशो ने महसूस किया कि संन्यास को एक नया जीवन, एक नई दृष्टि, एक नई चेतना दी जानी चाहिए। हिमालय में मनाली में अपने ध्यान शिविर के दौरान, भगवान कृष्ण की दिव्य चंचलता और जीवन के सभी रंगों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर बात करते हुए, ओशो ने युवा ध्यानियों के पहले समूह को दीक्षा देकर नवसंन्यास के एक नए युग की शुरुआत की थी। तब से संन्यास की ताज़ा हवा और इसकी ध्यानपूर्ण और सकारात्मक चंचल जीवनशैली पूरी दुनिया में बह रही है। ओशो, अपने जीवनकाल में कई बार हिमाचल प्रदेश आए। हिमाचल में उनकी यात्राएँ मुख्य रूप से आध्यात्मिक रिट्रीट और कम्यून स्थापित करने पर केंद्रित रहीं, जहां उनके अनुयायी ध्यान का अभ्यास कर सकते थे और आध्यात्मिकता और चेतना पर उनकी शिक्षाओं को समझ सकते थे। सन्यास पर ओशो ने दी नई व्याख्या ओशो ने कहा था संन्यास मेरे लिए त्याग नहीं, आनंद हैl संन्यास निषेध भी नहीं है, उपलब्धि है, लेकिन आज तक पृथ्वी पर संन्यास को निषेधात्मक अर्थों में ही देखा गया है, त्याग के अर्थों में, छोड़ने के अर्थों में, पाने के अर्थ में नहीं l मैं संन्यास को देखता हूं पाने के अर्थ में l निश्चित ही जब कोई हीरे जवाहरात पा लेता है तो कंकर पत्थरों को छोड़ देता है l लेकिन कंकर पत्थरों को छोड़ने का अर्थ इतना ही है कि हीरे जवाहरातों के लिए जगह बनानी पड़ती है l कंकर पत्थरों का त्याग नहीं किया जाता त्याग तो हम उसका करते हैं जिसका बहुत मूल्य मालूम होता है l कंकड़ पत्थर तो ऐसे छोड़े जाते हैं जैसे घर से कचरा फेंक दिया जाता है l घर से फेंके हुए कचरे का हिसाब नहीं रखते l संन्यास अब तक लेखा-जोखा रखता रहा उस सब का जो छोड़ा जाता है, मैं संन्यास को देखता हूं उस भाषा में, उस लेखे जोखे में जो पाया जाता है l यानी ओशो का ये नया संन्यासी संसार से दूर हिमालय की गुफाओं में नहीं बैठता, यह अपने घर में, दुकान में, बाज़ार के बिल्कुल बीच में खड़ा है और जीवन को एक अभिनय, एक लीला की तरह देखता है l यहाँ माना गया था की जब धरती पर अधिक से अधिक लोग इस भाव से जुड़ेंगे तब तनाव और हिंसा कम होती जायेगी और जीवन एक उत्सव बनता जाएगा l
हिमाचल के लिए वरदान साबित हुए भू -कानून, डॉ यशवंत सिंह परमार की सोच का नतीजा धार्मिक ग्रंथों से लेकर इतिहास की पोथियों तक ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि दुनिया में हुए महासंग्रामों में से अधिकतम के मूल में ज़मीन या उससे जुड़े विवाद रहे हैं। भूमि न सिर्फ समाज में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक है बल्कि यह उसकी जड़ों और उसके क्षेत्र से अपनत्व की भावना की भी परिचायक है। ज़मीन से जुड़ाव की भावना ही बहुतायत में राष्ट्रवाद जैसी धारणाओं को जन्म देती है। ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा ही सही, मगर अपना हो तो स्वाभिमान में बढ़ोतरी होना लाज़मी है। हिमाचल प्रदेश के बाशिंदों के इसी स्वाभिमान को कायम रखने की नींव भू-कानूनों के रूप में हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री और हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार ने रखी थी। देवभूमि कहे जाने वाले हमारे ख़ूबसूरत प्रदेश हिमाचल की तुलना अक्सर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से की जाती है, जो स्वयं भी देवभूमि की उपाधि से सुसज्जित है। ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर हिमाचल को उत्तराखंड से इक्कीस बताया जाता है, और इन्हीं में से एक है हिमाचल के भू-कानून। बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मुकाबले एक बेहतर राज्य के तौर पर उभरा है और इसका सबसे बड़ा कारण यही भू-कानून हैं। ये प्रदेश में लागू किए गए भू-कानून ही थे जिन्होंने हिमाचल को एक समृद्ध प्रदेश बनाया और हिमाचलवासियों के हितों को संरक्षित किया। यहाँ उत्तराखंड का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि भू-कानून से हिमाचल की सूरत कैसे बदली और ये हिमाचल के लिए वरदान क्यों साबित हुए, यह समझेंगे उस राज्य की परिस्थितियों से जहाँ ये कानून नहीं थे और जहाँ की जनता लंबे वक्त से हिमाचल की तर्ज पर भू-कानून और भूमि सुधारों की मांग कर रही है। आइए जानते हैं क्या हैं हिमाचल प्रदेश के भू-कानून, इनके पीछे की कहानी और ये कानून हिमाचल को समृद्धि के पथ पर आगे कैसे लेकर आए। इस कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से। हिमाचल प्रदेश को साल 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और देश के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल अस्तित्व में आया। यह वह वक्त था जब भू-बंदोबस्त, वनीकरण, बागवानी और कृषि जैसी कई दिक्कतें प्रदेश के सामने थीं। ज़मीनों पर भूमाफियाओं और धन्ना सेठों की नज़रें थीं। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार भविष्यद्रष्टा व्यक्तित्व के धनी थे और वह समय रहते इस समस्या को भांप गए। परमार समझते थे कि हिमाचल की जनता भोली है, अगर इनके अधिकारों को संरक्षित न किया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में यशवंत सिंह परमार ने विकास का जो मॉडल तैयार किया वो बाकी राज्यों के लिए उदाहरण बन गया। डॉ. परमार पहाड़ और पहाड़ियों के हितों के लिए हमेशा से संजीदगी के साथ सक्रिय रहे। कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और सूझ-बूझ से उन्होंने प्रदेश का इतिहास ही नहीं, भूगोल बदल डाला। बताया जाता है कि कुछ लोगों से मुलाकात के दौरान परमार को पता चला था कि जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची, वे उसी के यहाँ बतौर नौकर काम कर रहे हैं। इस पर परमार ने मंथन किया तो पाया कि अगर हिमाचल की ज़मीन पैसे वाले लोग खरीद लेंगे तो यहाँ के बाशिंदे सड़क पर आ जाएंगे। परमार ने अपने भाषण में कहा था कि पहले हिमाचल का युवा अन्य राज्यों में मज़दूरी करने जाया करता था, मगर अब हिमाचल इतना समृद्ध होगा कि किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। परमार समझते थे कि हिमाचल के पास सीमित भूमि है और इस क्षेत्र के लोगों की आय का सबसे बड़ा साधन यहाँ की भूमि पर होने वाली कृषि गतिविधियाँ ही होंगी और इसीलिए हिमाचल के छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए भू-कानून बनाए गए। 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के एक साल बाद ही प्रदेश में किरायेदारी और भूमि सुधार कानून लागू हो गया, जिसे हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 भी कहा जाता है। इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है धारा 118, जिसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति कृषि की ज़मीन निजी उपयोग के लिए नहीं खरीद सकता। धारा 118 के तहत ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर बहुत ही कड़े नियम-कायदे हैं। इसके तहत गैर-कृषकों को ज़मीन ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध है। यहाँ तक कि इस धारा के तहत हिमाचल में रहने वाला शख्स भी जो कृषक नहीं है या जिसके पास कृषि की भूमि नहीं है, वो भी कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश का कोई भी ज़मीन मालिक किसी भी गैर-कृषक को किसी भी ज़रिये (सेल डीड, गिफ्ट, लीज, ट्रांसफर, गिरवी आदि) से ज़मीन नहीं दे सकता। भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 2(2) के मुताबिक ज़मीन का मालिकाना हक उसका होगा जो हिमाचल प्रदेश में अपनी ज़मीन पर खेती करता होगा। जो व्यक्ति किसान नहीं है और हिमाचल में ज़मीन खरीदना चाहता है, उसे प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होगी। सरकार से अनुमति लेने पर मालिकाना हक मिल सकता है, लेकिन यह काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। उद्योग या पर्यटन से जुड़े विकास के मामलों में भी सरकार हर मसले और जानकारी की पूरी तरह से जांच-परख के बाद ज़मीन पर फ़ैसला लेती है। ज़मीन का चेंज लैंड यूज़ भी नहीं किया जा सकता। यानी ज़मीन अगर किसी अस्पताल के लिए ली गई तो उस पर मॉल या अन्य औद्योगिक इकाई नहीं लग सकती। फिर लैंड सीलिंग एक्ट में कोई भी व्यक्ति 150 बीघा ज़मीन से अधिक नहीं रख सकता। लीज को लेकर भी हिमाचल में कड़े नियम हैं। लीज या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़मीन भी किसी हिमाचली के नाम पर ही होगी। मौजूदा सुखविंदर सुक्खू सरकार ने लीज के वक्त को घटाकर 99 वर्ष से 40 साल कर दिया है। फरवरी 2023 में एक मामले की सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि हिमाचल प्रदेश में केवल किसान ही ज़मीन खरीद सकते हैं। अन्य लोगों को राज्य में ज़मीन खरीदने के लिए राज्य सरकार से इजाज़त लेनी होगी। 1972 के भूमि सुधार अधिनियम का हवाला देते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि "इसका उद्देश्य गरीबों की छोटी जोतों (कृषि भूमि) को बचाने के साथ-साथ कृषि योग्य भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए बदलने की जाँच करना भी है।" उत्तराखंड की स्थिति से समझे 118 का महत्व अब हिमाचल के भू-कानून क्यों ज़रूरी हैं, यह पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के हालातों से समझते हैं। उत्तराखंड में ग्रामीण इलाकों में साधनहीन लोग धन के अभाव में अपनी ज़मीन बेच देते हैं। फिर वे लैंडलेस हो जाते हैं। सख़्त भूमि कानून के अभाव में उत्तराखंड के जंगल भी ख़तरे में हैं और पलायन का कारण भी उत्तराखंड में यही रहा कि खेती से वहाँ रोज़गार के खास प्रयास नहीं हुए। उत्तराखंड में इन्हीं कारणों से गाँव बचाओ यात्रा जैसे आंदोलन भी हुए। उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति भी अपनी पहचान बनाए रखना चाहती है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग यदि उत्तराखंड में बिना रोक-टोक ज़मीन खरीदते रहेंगे तो यहाँ के सीमांत और छोटे किसान भूमिहीन हो सकते हैं। हिमाचल ने इस संकट को अपने अस्तित्व में आने पर ही पहचान लिया था और हिमाचल ने अपनी ज़मीन बचाने के लिए शुरू से ही काम किया है। धारा-118 के साथ छेड़छाड़ की कोई भी राजनीतिक दल सोच भी नहीं सकता। यहाँ की जनता जागरूक है और भूमि सुधार कानून के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करती। हिमाचल प्रदेश निर्माता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाई. एस. परमार ने ऐसे कानूनों की नींव रखी कि हिमाचल की भूमि बाहरी लोग न ले पाएं। यहाँ बाहरी राज्यों के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। यही कारण है कि हिमाचल में बाहरी राज्यों के प्रभावशाली लोग ना के बराबर ज़मीन खरीद पाए हैं। बेशकीमती कृषि और बागवानी भूमि को धन्ना सेठों के हाथों बिकने से बचाकर ही हिमाचल अपना वजूद कायम रख पाया है। हालाँकि अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी इस दिशा में पहल ज़रूर की है। हिमाचल में कैसे खरीद सकते हैं ज़मीन धारा-118 में ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जो किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति को आधिकारिक सहमति के अनुरोध के बाद हिमाचल प्रदेश में भूमि और संपत्ति दोनों खरीदने की मंज़ूरी देती हैं। बता दें कि यहाँ भूमि शब्द का मतलब कृषि योग्य क़ब्ज़े वाली या पट्टे पर दी गई ज़मीन से है। बाहरी राज्य के व्यक्ति को भूमि खरीद के लिए एक आवेदन जमा करना होगा। इसमें उसे कारण बताना होगा कि वह भूमि किस उद्देश्य के लिए खरीद रहा है। राज्य सरकार आवेदक की ओर से उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों की जांच व पुष्टि करने के बाद फ़ैसला लेती है कि व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है या नहीं। इसी प्रक्रिया के तहत शिमला में कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने भी ज़मीन ली है।
"अरख मनीमा किन्नौरु संस्कृति खानंग", यानी देसी शराब के बिना किन्नौर की संस्कृति अधूरी है। यह कोई कहावत नहीं, बल्कि किन्नौर की पहाड़ियों में बसे गांवों की ज़मीनी सच्चाई है, जहां देसी सुरा केवल एक पेय नहीं, बल्कि जीवन, परंपरा और आस्था का हिस्सा है। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में गिना जाता है जो आज भी अपनी लोक संस्कृति, धार्मिक रीति-रिवाज़ों और पारंपरिक मान्यताओं को ज्यों का त्यों संजोए हुए है। यहां की घाटियों में बहती शीतल हवा, बर्फ से ढके पहाड़, और हर ओर गूंजती देवताओं की जयघोष के बीच देसी सुरा का विशेष स्थान है। देसी सुरा, जिसे स्थानीय भाषा में अरख या चंग भी कहा जाता है, केवल पीने की चीज नहीं बल्कि पूजा का प्रमुख अंग है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान, पारिवारिक आयोजन या सामूहिक उत्सव होता है, सुरा को सबसे पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है। यह सुरा “प्रसाद” बन जाती है, और फिर समाज के लोग इसे पूरे श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं। घर में नया निर्माण हो, खेतों में पहली फसल लगे, विवाह की बात पक्की करनी हो या फिर नवजात का स्वागत, हर शुभ अवसर पर सुरा का प्रयोग आशीर्वाद और समर्पण के प्रतीक के रूप में किया जाता है। किन्नौर में सुरा बनाना केवल घरेलू प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान है। महिलाएं पारंपरिक विधियों से इसका निर्माण करती हैं। अंगूर, सेब, चुल्ली और खुमानी, गेहूं या जौ को कुछ विशेष स्थानीय जड़ी-बूटियों के साथ किण्वित किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया पवित्रता और अनुशासन के साथ की जाती है। यानी साफ सफाई का सख्ती से पालन किया जाता है। इसे मिट्टी के बर्तनों में या लकड़ी के खास पात्रों में कई दिनों तक रखा जाता है ताकि इसका स्वाद और असर संतुलित रहे। इस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली जड़ी-बूटियों को भी आयुर्वेदिक दृष्टि से लाभकारी माना जाता है। कई लोग इसे देवताओं का पेय कहते हैं, और यह मान्यता कि यह शरीर को गर्माहट और बल प्रदान करती है, आज भी यहां जीवित है। रिश्तों की शुरुआत भी सुरा से किन्नौर में रिश्तों की शुरुआत भी सुरा से ही होती है। जी, हां! किन्नौर की एक अनूठी सामाजिक परंपरा है, रिश्ता पक्का करने के लिए सुरा भेजना। जब किसी लड़के का परिवार किसी लड़की से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजता है, तो वे साथ में देसी सुरा भेंट स्वरूप भेजते हैं। यदि लड़की का परिवार इसे स्वीकार कर लेता है, तो यह संकेत होता है कि रिश्ता तय हो गया। यह रिवाज़ केवल एक सामाजिक स्वीकृति नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, विश्वास और मर्यादा का प्रतीक है। आज भी यह परंपरा उतनी ही जीवित है जितनी दशकों पहले थी। पर्व, परंपरा और प्रसाद किन्नौर में फागुली, फुआयच मेला, लोसार, राउलाने जैसे त्योहारों के मौके पर जब गांव के लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजते हैं, देवताओं के सम्मान में नृत्य करते हैं और लोकगीत गाते हैं, तब सुरा को प्रसाद के रूप में सभी में बांटा जाता है। सुरा यहां उत्सवों का रस है। बिना इसके कोई पर्व अधूरा लगता है। कई बुज़ुर्ग तो यहां तक कहते हैं कि “देवता सुरा के बिना पूजा स्वीकार ही नहीं करते।” बाजार से दूर, परंपरा के पास देसी सुरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यापार का हिस्सा नहीं है। इसे न बेचा जाता है, न इसका कोई विज्ञापन होता है। यह पूरी तरह से घरेलू, धार्मिक और सांस्कृतिक उपयोग के लिए बनाई जाती है। यही कारण है कि आज भी यह परंपरा मूल रूप में जीवित है। स्थानीय महिला रिंगचेन नेगी कहते हैं कि हम सुरा को कोई आम शराब नहीं मानते। ये हमारी परंपरा की धरोहर है। अगर हम इसे नहीं निभाएंगे, तो संस्कृति बचेगी कैसे? वहीं, युवतियां भी सुरा बनाने की पारंपरिक विधियां सीख रही हैं ताकि यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके।
मान्यता : सोने-चांदी-ताबे-लोहे के 4 अदृश्य दरवाजे देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर को शिव नगरी कहा जाता है। इसी शिव नगरी भरमौर में स्थित है चौरासी मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर में साक्षात यमराज विराजमान हैं। माना जाता है कि यहां यमराज की अदालत लगती है और यहीं से यह तय होता है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक जाएगा या नर्क लोक। ये मंदिर बाहर से देखने में बिलकुल आम नजर आता है, लेकिन इसकी मान्यता सबसे अनूठी है। कहा तो यह भी जाता है कि इस मंदिर में चार अलग-अलग धातु के अदृश्य दरवाजे भी हैं और यह द्वार सोना, चांदी, तांबे और लोहे से बने हुए हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में चार दिशाओं में चार द्वार का उल्लेख किया गया है। चौरासी मंदिर संसार के इकलौते धर्मराज महाराज या मौत के देवता का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना के बाबत किसी को भी सही जानकारी नहीं है। बस इतना जरूर है कि चंबा रियासत के राजा मेरू वर्मन ने छठी शताब्दी में इस मंदिर की सीढिय़ों का जीर्णोद्धार किया था। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कमरा माना जाता है। चित्रगुप्त जीवात्मा के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। दरअसल हिन्दू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब धर्मराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़ कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा लेखा-जोखा देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। फिर यमराज व्यक्ति की आत्मा का भविष्य का रास्ता तय करते हैं। इस बात का जिक्र गरुड़ पुराण में भी किया गया है। मान्यता है कि इसी मंदिर में यमराज की कचहरी लगती है और कर्मों के आधार पर फैसला आता है। मुक्ति धाम के नाम से विख्यात शिव नगरी भरमौर जिसे भगवान शंकर की चरणस्थली भी कहा जाता है। ऐसी जनश्रुति है कि भगवान शंकर के त्रिशूल पर काशी को विराजमान माना जाता है तो चरणस्थली चौरासी मानी जाती है। काशी में मात्र विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने सभी पापों का अंत हो जाता है तो चौरासी के दर्शन करने से 84,000 योनियों के चक्कर से छुटकारा मिलता है। भगवान सूर्य की संतान हैं यमराज और यमुना भाई दूज के त्योहार के दिन यहां भक्तों की भारी भीड़ लगती है। मान्यता है कि इस दिन यमराज से मिलने उनकी बहन यमुना इस मंदिर में आती हैं। पौराणिक कथाओं में यमराज और यमुना को भगवान सूर्य की संतान बताया गया है। कुछ लोग इसे सिर्फ कहानी मात्र ही मानते हैं और कुछ लोगों का समानता पर अटूट विश्वास है। पिंड दान के लिए दूर-दूर से आते हैं लोग स्थानीय लोगों के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मौत हो जाती है, तो उसके सगे-संबंधी यहां पिंड दान के लिए आते हैं। मंदिर के पास ही वैतरणी नदी भी बहती है, जहां गौ-दान किया जाता है।
अनोखी मान्यता : इस मंदिर से बाहर आते समय नहीं बोल सकते हैं 'चलो' मां मृकुला देवी मंदिर आस्था, रहस्य और रोमांच का अद्धभूत संगम हैं। लाहौल घाटी के उदयपुर में स्थित मृकुला देवी मंदिर में मां काली की महिषासुर मर्दिनी के आठ भुजाओं वाले रूप में पूजा की जाती है। कश्मीरी कन्नौज शैली में बना हुआ ये मंदिर कई रहस्यों और दंतकथाओं का जीवंत उदाहरण है। मान्यता है कि महिषासुर का वध करने के बाद मां काली ने यहीं पर खून से भरा हुआ खप्पर रखा था। यह खप्पर आज भी यहां मुख्य मूर्ति के पीछे रखा हुआ है, जिसे किसी को देखने की अनुमति नहीं है। लोगों में आस्था है कि अगर इस खप्पर को कोई गलती से भी देख ले तो वह अंधा हो जाता है। आज भी लोग इस खप्पर को देखने का साहस नहीं करते। लाहुल घाटी में साल में एक बार फागली उत्सव होता है। उत्सव की पूर्व संध्या पर मां मृकुला देवी मंदिर के पुजारी खप्पर की पूजा-अर्चना की रस्म अदायगी अकेले करते हैं। तब खप्पर को बाहर निकाला जाता है, लेकिन कोई देखता नहीं है। बुजुर्गों की बात पर यकीन किया जाए तो 1905-06 में इस खप्पर को देखने वाले चार लोगों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। आज भी यह परंपरा कायम है और कोई भी उस खप्पर को नहीं देखता। लोकश्रुति के अनुसार महाबली भीम एक दिन एक विशालकाय पेड़ को यहां लाए और उन्होंने देवता के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा से यहां मंदिर के निर्माण के लिए कहा और विश्वकर्मा ने एक दिन में इस मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के भीतर बनी कलाकृतियां अद्धभूत हैं, चाहे कहीं मृत्यु शैया में लेटे भीष्म पितामह हो, सागर मंथन, सीता मैया का हरण, अशोक वाटिका, द्रोपदी स्वयंवर, चक्रव्यूह या कोई अन्य कलाकृति। इस मंदिर का रखरखाव भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। हिंदू इस मंदिर में मृकुला देवी या देवी काली की पूजा करते हैं, वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे वज्रराही देवी (एक क्रोधित बौद्ध देवी) के रूप में पूजते हैं। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि इस स्थान पर तांत्रिक संत पद्मसंभव ने साधना की थी। 'चलो' कहना मना है मंदिर कपाट के पास दो द्वारपाल, बजरंग बली और भैरो देव तैनात हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं को बताया जाता है कि यहां पूजा-अर्चना और दर्शन के बाद भूलकर भी ‘चलो यहां से चलते हैं’ नहीं बोल सकते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा कहने पर उनके घरों में अशुभ घटनाएं घट सकती हैं। बताते हैं कि ऐसा कहने पर इस मंदिर के द्वार पर खड़े दोनों द्वारपाल भी साथ चल पड़ते हैं। स्थानीय लोग बताते है कि 'कई साल पहले एक परिवार के सदस्य दर्शन के बाद "चलो चलो घर चलो" कहकर निकल गए थे, जिससे द्वारपाल भी उनके साथ चले गए। इसके बाद उनके घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं, जब उन्होंने देवता से सलाह ली, तो उन्हें मंदिर लौटकर क्षमा याचना करनी पड़ी, तभी जाकर उनके घर में शांति लौटी। आज भी बाहर से आने वाले सैलानियों को इन नियमों की जानकारी पहले ही दे दी जाती है।' ढाई मन वजनी पत्थर के बराबर मिलता था भीम को भोजन मंदिर प्रांगण में करीब ढाई मन वजनी एक पत्थर है जिसे उठाना तो दूर हिलाने में भी पसीने छूट जाते हैं। बताते हैं कि सच्चे मन से मां के जयकारों के साथ पांच या सात लोग एक मध्यम उंगली से इस पत्थर को बड़ी सुगमता से हिला या उठा सकते हैं। कहते है यह पत्थर भीम के लिए रखा गया था। भीम पांडवों का सारा भोजन चट कर जाते थे, ऐसे में उन्हें इस पत्थर के वजन के बराबर एक समय का भोजन ही दिया जाता था ताकि शेष लोगों के भोजन हेतु कुछ बच सके। मरगुल से उदयपुर हुआ नाम बताते हैं कि 16वीं शताब्दी से पहले इस गांव का नाम मरगुल था। तब चंबा के राजा उदय सिंह लाहौल आए। उन्होंने देवी की अष्टधातु की मूर्ति की स्थापना की। इसके बाद गांव का नाम उदयपुर पड़ गया। यह गांव तांदी- किश्तवाड़ मार्ग पर चिनाब (चंद्रा और भागा) नदी के किनारे बसा है।
सेहत, संस्कृति और जनजातीय संस्कृति की परिचायक है 'बटर टी' जब हम चाय का ज़िक्र करते हैं, तो ज़हन में सबसे पहले मीठी, दूध वाली चाय की तस्वीर उभरती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों खासकर स्पीति और किन्नौर में चाय का एक अनोखा और दिलचस्प रूप है, नमकीन चाय, जिसे स्थानीय भाषा में छा चा या बटर टी भी कहा जाता है। यह चाय जितनी साधारण दिखती है, उतनी ही गहराई से संस्कृति, भूगोल और जीवनशैली से जुड़ी हुई है। भारत में जहाँ चाय का मतलब आमतौर पर दूध और चीनी से बनी मीठी चाय होता है, वहीं किन्नौर और स्पीति में चाय का मतलब होता है मक्खन, नमक, चायपत्ती और कभी-कभी याक के दूध का मेल। यह चाय शरीर को ऊर्जा देती है, ठंड में गर्मी बनाए रखती है और ऊँचाई पर ऑक्सीजन की कमी से लड़ने में मदद करती है। यकीन मानिये यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं, बल्कि स्थानीय ज्ञान का परिणाम है या ऐसा कहें एक ऐसा समाधान जो सदियों पहले वहां के लोगों ने कठिन मौसम से जूझने के लिए खोजा था। लकड़ी के थर्मस में बनाई जारी है यह विशेष चाय नमकीन चाय को बनाने का तरीका भी उतना ही खास है जितना उसका स्वाद। इसे तैयार करने के लिए स्थानीय लोग एक विशेष लकड़ी के पात्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसे चांगमो कहा जाता है। यानि यह लकड़ी से बनाया गया बटर टी चर्नर है। यह एक तरह का परंपरागत थर्मस है जिसमें चाय को डालकर लंबे समय तक फेंटा जाता है। इस प्रक्रिया से चाय में झाग बनती है और उसकी बनावट गाढ़ी व मुलायम हो जाती है। चांगमो सिर्फ एक बर्तन नहीं, एक पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है, जिसे हर घर में सहेज कर रखा जाता है, जिसकी कीमत नक्काशी के आधार पर 5000 से लेकर 5 लाख तक होती है। नमकीन चाय बनाने के लिए बाजार में मिलने वाली चायपत्ती का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि चाय पट्टी के तौर पर लकड़ी के टुकड़े को उबला जाता है। इस चाय के लिए पहाड़ो से निकली गयी प्राकृतिक शिंग चा यानी पहाड़ो में पाई जाने वाली लकड़ी चाय को एक स्पेशल कपड़े में बांधकर पानी के बर्तन में चाय के रंग आते तक रखा जाता है और पानी को करीब आधा घण्टा उबाला जाता है। बाज़ार में आसानी से अवेलेबल नहीं होने के चलते इसकी डिमांड और अधिक बढ़ जाती है। चाय नहीं, मेहमान-नवाज़ी की पहली सीढ़ी किन्नौर और स्पीति में अगर आप किसी घर जाएँ, तो सबसे पहले जो चीज़ आपके हाथ में दी जाएगी, वह है नमकीन चाय की प्याली। यह शाही मेहमाननवाजी का हिस्सा है। यहाँ यह नहीं पूछा जाता कि चाय लेंगे, बल्कि सीधे परम्परागत तरीके से बनाई गयी "लो हाइट टेबल" जिसे "चोकचे" कहा जाता है पर परोसा जाता है। होटलों की ट्रे तक पहुँची यह परंपरा आज यह चाय सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रही। जैसे-जैसे पर्यटन ने रफ्तार पकड़ी है, वैसे-वैसे नमकीन चाय पर्यटकों के बीच एक विशेष आकर्षण बन गई है। स्पीति और किन्नौर के होटलों, होमस्टे और लोकल कैफे में अब इसे खास तौर पर पेश किया जा रहा है, वो भी अच्छे खासे रेट पर। विदेशी सैलानी इसे ‘Himalayan Butter Tea’ के नाम से पहचानते हैं और भारतीय पर्यटक इसे एक नई संस्कृति से जुड़ने का अनुभव मानते हैं। होटल संचालक सुमित नेगी बताते है कि यह चाय अब एक लोकल डिलाइट नहीं, बल्कि एक संस्कृति से संवाद का माध्यम बन चुकी है। नेगी बताते है कि आज के दौर में जब बहुत सी पारंपरिक चीजें गुम हो रही हैं, नमकीन चाय ने खुद को समय के साथ जोड़ लिया है लेकिन अपनी जड़ों से कटे बिना। यह अब सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है।
‘पूर्ण भक्त’ नाटक के लिए आए थे शिमला, महान संगीतकार हरिशचंद्र बाली ने पहचानी प्रतिभा साल था 1935, सिल्वर स्क्रीन पर देवदास फिल्म की धूम थी और इसमें मुख्य किरदार निभाने वाले कुंदन लाल सहगल फिल्म उद्योग के पहले सुपरस्टार बन गए। इसके बाद कुंदन लाल सहगल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शौहरत की बुलंदियां छूते चले गए। हिंदी सिनेमा के इस पहले सुपर स्टार का शिमला से गहरा नाता रहा है। साल 1928 में जम्मू से शिमला आने वाले कुंदन लाल सहगल के अभिनय और गायकी को गेयटी थियेटर शिमला और एमेच्योर ड्रामाटिक क्लब फागली ने पहचान दी। उन्हें फिल्मों में गाने का ब्रेक भी शिमला में मिला। 1928 में एमेच्योर ड्रामाटिक क्लब फागली ने कुंदन लाल सहगल को 'पूर्ण भक्त' नामक नाटक के मंचन के लिए शिमला बुलाया था। दरअसल नाटक में मुख्य भूमिका अदा करने वाले अभिनेता और गायक डायरिया के चलते बीमार पड़ गए। तब किसी ने कुंदन लाल सहगल का नाम सुझाया। सहगल नाटक देखने के लिए नियमित रूप से आते थे, इसलिए उन्हें नाटक की पंक्तियाँ और गाने याद थे। इसके साथ ही शुरू हुआ सहगल का दौर। नाटक को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला और दर्शक सहगल की अदाकरी और आवाज के मुरीद हो गए। इस दौरान एक दिन जब वे गियेटी थियेटर के मंच पर गायन की प्रस्तुति दे रहे थे तो महान शास्त्रीय संगीतकार हरिशचंद्र बाली की निगाह उन पर पड़ी। वे सहगल को अपने साथ कलकता ले गए और फिल्म संगीत के जनक रायचंद बोरल से मिलवाया। सहगल और बीआर सरकार के स्टूडियो ‘न्यू थियेटर’ ने गायन के लिए करार हुआ और देखते ही देखते पूरा हिंदुस्तान उनकी गायकी का मुरीद हो गया। शिमला में रहते हुए कुंदन लाल सहगल भराड़ी के कोडुमल भवन में रहते थे। दिलचस्प बात ये है उन्होंने साल 1928 से साल 1931 तक रेमिंगटन रैंड टाइपराइटर कंपनी में एक टाइपराइटर विक्रेता के रूप में कार्य किया। रेमिंगटन टाइपराइटर के विपणन का कार्य शिमला की ठाकर, स्पिंक एंड कंपनी करती थी जो किताबें, पोस्टर और तस्वीरें प्रकाशित करने का काम करती थी। कंपनी का कॉम्बेरमेयर ब्रिज के पास इमारत में फोटोग्राफिक स्टूडियो था। देवदास फिल्म की सफलता के बाद साल 1936 में सहगल फिर शिमला आए और उनके सम्मान में समारोह हुआ। तब वह होटल ग्रांड में रूके। उनके सम्मान में कालीबाड़ी हॉल में एक चैरिटी शो आयोजित किया गया। सहगल ने अपने गीतों से शिमला का दिल जीत लिया। 18 जनवरी 1947 को जालंधर में 42 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। महाराजा राजेंद्र सिंह देव बहादुर ने उपहार में दिया सूट गेयटी में एक नाटक में कुंदन लाल सहगल ने एक हिजड़े की भूमिका निभाई और गाया, "सैयां मोरे लाए रे बताशे की जोरी।" उनकी अदाकारी और गायकी स्थानीय लोगों के सर चढ़कर बोलने लगी। इत्तेफ़ाक़ से झालावाड़ के महाराजा राजेंद्र सिंह देव बहादुर ने भी उनकी ये परफॉरमेंस देखि और वे केएल सहगल से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मॉल, शिमला के 'रैंकेन एंड कंपनी-टेलर्स एंड ड्रेपर्स' से खरीदा गया एक बहुत महंगा सूट उन्हें उपहार में दे दिया । रेडियो सीलोन पर सात बज कर 57 मिनट पर बजता था सहगल का गीत अपने दो दशक के सिने करियर में सहगल ने 36 फिल्मों में अभिनय किया, लगभग 185 गीत गाए, जिनमें 142 फिल्मी और 43 गैर-फिल्मी गीत शामिल हैं। सहगल 18 जनवरी, 1947 को केवल 43 वर्ष की उम्र में इस संसार को अलविदा कह गए थे। सहगल की आवाज की लोकप्रियता का यह आलम था कि कभी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा रेडियो सीलोन कई साल तक हर सुबह सात बज कर 57 मिनट पर इस गायक का गीत बजाता था। रवीन्द्र संगीत गाने वाले पहले गैर बांग्ला गायक रवीन्द्र संगीत गाने का सम्मान पाने वाले पहले गैर बांग्ला गायक थे। उस दौर में भारतीय फिल्म उद्योग मुंबई में नहीं बल्कि कलकत्ता में केंद्रित था। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस जमाने में उनकी शैली में गाना अपने आपमें सफलता की गारंटी मानी जाती थी। मुकेश और किशोर कुमार ने अपने करियर के आरंभ में सहगल की शैली में गायन किया भी था।
जीणा कांगड़े दा : भीड़ की गारंटी थी प्रताप शर्मा की आवाज के साथ धंतारू अलबत्ता, 'जीणा कांगड़े दा...', सहित दर्जनों लोकगीतों को अपनी मधुर आवाज देकर जन-जन तक पहुंचाने वाले प्रसिद्ध लोकगायक प्रताप चंद शर्मा का देहावसान हुए कई बरस बीत गए हो, पर उनके लोक गीत आज भी कांगड़ा सहित हिमाचल के कोने कोने में अपना जादू बिखेर रहे है। तो क्या हुआ उनका एक इकतारा या धंतारू अब खामोश है और अकेला भी , किन्तु उनकी संगीतमय विरासत तो हिमाचल की सांस्कृतिक आवो हवा में खुशबू की तरह घुली है। इस खुशबू को तो हुकुमरानों की उपेक्षा भी विरल न कर सकी। एक दौर में प्रताप चंद शर्मा की आवाज के साथ धंतारू, भीड़ की गारंटी थी। विशेषकर 60 के दशक में उनका लिखा गया 'गीत ठंड़ी-ठंडी हवा झुलदी, झुलदे चीलां दे डालू, जीणा कांगड़े दा' जब उनकी ही आवाज में आया था, तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। ये गीत न सिर्फ उनका ट्रेडमार्क बन गया बल्कि आज भी कांगड़ा के संगीत की पहचान है। इस कदर प्यार शायद ही किसी और पहाड़ी गीत को मिला हो। प्रताप चंद शर्मा ने करीब 200 गीत लिखे थे, और सब बेमिसाल। इनके लिखे कई पहाड़ी गीत आज लोकगीत बन गए हैं। स्वर्गीय लोक गायक प्रताप चंद शर्मा ने 'मेरी धरती, मेरे गीत' किताब भी लिखी है, जिसमें 120 गाने हैं। उनके गीत गाकर कई कलाकारों ने लूटी शौहरत अब जो कांगड़ी गीत संगीत सर्वाधिक चर्चित होकर चलन में है, उसका बड़ा हिस्सा प्रताप चंद शर्मा का रचा-गाया हुआ है। कांगड़ा क्षेत्र में गांव गांव घूम कर उन्होंने अपने अनूठे गीतों का प्रसार किया ही, प्रदेश और देश के दूसरे अंचलों में भी कांगड़ा की ठंडी-ठंडी हवा का संगीत यहां की प्रकृति और जीवन के रंगों के साथ पहुंचा दिया है। प्रताप चंद शर्मा ने ठंडी-ठंडी हवा झुलदी, झुलदे चीलां दे डालू, दो नारां वे लोको लश्कदियां तलवारां, जे तू चला नेफा नौकरी, मेरे गले दे हारे लैंदा ओयां, नाले पार गीतां जो जाणां विच विहाए नचणा गाणा चा नाचे दा, असां क्या गलाया तां तिजो गुस्सा आया व कमला विमला जुड़वां भैणां दोहे इकयी नुहारी जी सहित कई गीत लिखे और गाए जो लोगों की जुबां पर आ गए। उनके लिखे गीत गाकर कई गायकों ने शौहरत लूटी, किसी ने वाइस करेक्शन का सहारा लिया है तो किसी के अन्य आधुनिक तकनीकों का। पर कोई उनके स्तर को छू न सका। खुद तैयार किया इकतारा, पिता से सीखी बारीकियां लोकगायन के प्रति प्रताप चंद शर्मा की साधना का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने खुद लोकवाद्य इकतारा जिसे स्थानीय भाषा में धंतारू कहते हैं, बना कर उस पर कई कालजयी धुनों की रचना की। प्रताप शर्मा ने गांवों में गाई जाने वाली राग- रागणियों का अध्ययन किया और कई नायाब गीत लिखे। प्रताप चंद शर्मा के पंडित झाणुराम खेती करने के साथ कथा- कीर्तण भी करते थे और लोक संगीत के अच्छे जानकार थे। पिता की संगत में ही उन्हें संगीत का चस्का लग गया। पिता को भी उनमें प्रतिभा दिखी, तो लोकगायकी के गुर सिखाए। जब महिंद्र कपूर ने गाना छोड़ माइक थमा दिया चर्चित किस्सा है कि एक बार हमीर उत्सव में मुंबई से शैलेंद्र सिंह और महिंद्र कपूर सरीखे नामी बॉलीवुड गायक भाग लेने आए थे। इस उत्सव में प्रताप शर्मा भी मौजूद थे। प्रताप चंद शर्मा को चाहने वालो ने उनके नाम की हूटिंग शुरू कर दी, जिसके बाद महिन्द्र कपूर ने माइक प्रताप शर्मा को थमा आइये और खुद एक श्रोता बन कर कार्यक्रम का आनंद लिया। उपेक्षा झेलता रहा लोक संस्कृति का ध्वजवाहक 23 जनवरी 1927 को नलेटी, देहरा में जन्मे प्रताप चंद शर्मा का निधन 92 साल की आयु में साल 2018 में हुआ था। पहाड़ी गीतों को हर जुबां तक लाने वाले स्व. प्रताप चंद शर्मा को जीते जी तो सरकारी स्तर पर वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वह हकदार थे। उनकी नौकरी लगातार अनुबंध पर रही जो उन्हें पेंशन का हकदार नहीं बना सकी। प्रताप चंद शर्मा सम्मान बहुत मिले लेकिन सिर्फ सम्मान से घर गृहस्थी कहाँ चलती है ? 1962-1986 तक लोक संपर्क विभाग कांगड़ा के अनुबंध कर्मचारी रहे। उन्हें कार्यक्रम के हिसाब से भुगतान किया जाता था। शुरू में हर कार्यक्रम के लिए पाँच रुपये मिलते थे, जो दशकों बाद 400 रुपये प्रति कार्यक्रम तक पहुंचे थे। एक इंटरव्यू में प्रताप चंद शर्मा ने कहा था, " मैंने लोक संपर्क विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए कई गीत रचे और गाए पर विभाग की तरफ से पैंशन नहीं मिली। इस बात का मलाल है। पर हिमाचल की जनता से मुझे बहुत प्यार मिला। " इससे भी अधिक शर्मिंदगी इस बात ये है कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी उपेक्षा खत्म नहीं हुई। हिमाचल संस्कृति के ध्वजवाहक रहे प्रताप चंद शर्मा की अंत्येष्टि में प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा था। इस बीच प्रताप चंद शर्मा की पत्नी सत्या देवी की उम्र अब 92 बरस हो गई है। पति को गुजरे सात साल बीत चुके है लेकिन सत्या देवी इसी आस में है कि सरकार से प्रताप चंद शर्मा को जो मान -सम्मान जीत जी हासिल न हुआ, वो अब मिल जाए। देहरा में उनकी एक मूर्ति ही लग जाए ताकि उनसे जुड़ी स्मृतियां ही बची रहें, और आने वाली पीढ़ी भी इस कर्मयोगी को याद रखे।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जोगिंद्रनगर में अंग्रेजों के जमाने का एक पावर प्रोजेक्ट है जिसे शानन पावर प्रोजेक्ट ने नाम से जाना जाता है। शानन परियोजना को स्थापित करने के लिए 3 मार्च, 1925 को तत्कालीन पंजाब सरकार तथा मंडी के राजा के बीच समझौता हुआ था। 99 साल की लीज पर ये पंजाब सरकार के पास था और फिलवक्त हिमाचल सरकार इस पर कब्जे को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही है। इस पावर प्रोजेक्ट का निर्माण ब्रिटिश राज में हुआ था और उस दौर इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए अंग्रेजों ने खड़ी पहाड़ी पर रेलवे ट्रैक तैयार करवा दिया था, जो आज भी अद्धभूत है। यह रेलवे ट्रैक खड़ी पहाड़ी से जब गुजरता है तो इस पर चलने वाली ट्राली में बैठे लोगों की सांसें थमने लग जाती हैं। दरसल बरोट में बांध बनाने के लिए 1926 में अंग्रेज इंजीनियर कर्नल बैटी ने एक रोप-वे ट्रॉली (हॉलेज ट्रॉली) का निर्माण किया था। इस ट्रॉली के जरिए बांध का सारा सामान जोगिन्द्र नगर से बरोट पहुंचाया गया था। यह ट्रॉली आज भी कार्य करती है। इसकी खासियत यह है कि यह बिना किसी इंजन के सहारे काम करती है। ये ट्रैक लगभग 9 किलोमीटर लम्बा है। वर्तमान में यह ट्रॉली जोगिंद्रनगर के शानन पावर हाउस से बैंच कैंप, हैडगियर, कथयाडू (यह ट्रॉली का कंट्रोल प्वाइंट है) व जीरो प्वाइंट तक चलती है। पहले यह ट्रॉली बांध तक थी। कथयाडू से लेकर जीरो प्वाइंट के रास्ते को खूनी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां ट्रॉली लगभग 90 डिग्री के कोण पर चलती है।
मोहरों पर बैठती है मधुमक्खी तब माना जाता है श्री शेषनाग जी का शक्ति अर्जन पूर्ण देवभूमि हिमाचल के लोगों के लिए देवी-देवता केवल आराध्य नहीं, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक भी हैं। देवता की शक्ति के आगे हर हिमाचली पूरी श्रद्धा से नतमस्तक होता है और हिमाचल की ये देव परम्पराएं यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोए हुए है। अटूट श्रद्धा का केंद्र ऐसे ही देवता है जीभी घाटी के अधिष्ठाता गढ़पति श्री शेषनाग जी महाराज, सहज स्वभाव वाले मगर अत्यंत शक्तिशाली। ये देवता मधुमक्खियों के जरिये साक्षात चमत्कार दिखाते हैं। दरअसल हर 12 से 18 साल में श्री शेषनाग जी महाराज हर 12 से 18 साल में अपने हजारों हरियानों के साथ जगती-बाल्य बीढ़ पर शक्ति अर्जित करने जाते हैं, जहां से ठीक सामने मूल माहूँनाग का स्थान नजर आता है। माहूँ (मधुमक्खी), जब श्री शेषनाग जी महाराज के मोहरों पर आकर बैठती हैं तब माना जाता है कि उनका शक्ति अर्जन पूर्ण हुआ। इन्द्रप्रस्थ में प्रकट हुए, फिर जीभी पहुंचे मान्यता है कि द्वापर युग में श्री शेषनाग जी महाराज सबसे पहले इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली) में प्रकट हुए और फिर वहां से उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्तान किया। इसी दौरान वे हुए मंडी के मूल माहूँनाग पहुंचे और वहां अपनी जेरठी- यानी ज्येष्ठ कला स्थापित की। तदोपरांत श्री शेषनाग जी महाराज आनी की बाल्य बीढ़ नामक जगती पर पहुंचे और फिर बंजार के जीभी में आकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि जीभी का नाम भी देवता शेषनाग जी के मंदिर के स्थान के कारण ही पड़ा है, क्योंकि मंदिर के दोनों ओर दो खड्ड बहती हैं और बीच का स्थान पर जीभ जैसी आकृति दिखाई देती है। बैसाख की संक्रांति से लेकर 7 बैसाख तक श्री शेषनाग जी महाराज के मेले मनाए जाते हैं। वहीँ साल में दो बार देवता जी सभी हारियों की परिक्रमा करते हैं- जिनमें मूल माहूँनाग, धींजू, लाम्बा लाम्ब्री की जोगनी, सर्योल्सर, जगतपुर गढ़ और जोगी पाथर शामिल हैं।
मुसाधा : लोक गाथा गायन की भी समृद्ध परंपरा हिमाचल लोकसाहित्य की अनेक विधाओं में लोक गाथा गायन की भी समृद्ध परंपरा है। इन विधाओं में चंबा जिला की सांस्कृतिक विरासत मुसाधा गायन का विशेष स्थान है। पूर्ण रुप से धार्मिक परंपराओं से जुड़े मुसाधा गायन में दो कलाकार होते हैं। पुरुष कलाकार को ‘घुराई’ और स्त्री कलाकार को ‘घुरैण’ कहते हैं। मुसाधा लोक कलाकार शायद विश्व में पहला लोक कलाकार है जो एक साथ दो वाद्य यंत्रों को बजाते हुए गाता है। एक हाथ में वाद्ययंत्र खंजरी से ताल बजाता है और दूसरे हाथ से गले में लटका वाद्य यंत्र रुबा (तार वाद्य) से संगीत देते हुए गाता है। घुरैण (स्त्री कलाकार) हाथों में कंसी बजाते हुए गाने में साथ देती है। मुसाधा में रामायण, महाभारत, शिव पुराण इत्यादि का गाथा गायन किया जाता है और प्रसंग गाने के उपरांत बीच-बीच में स्थानीय भाषा में उसकी व्याख्या कथा के रूप में की जाती है। मुसाधा का आयोजन भगवान शिव के निमित्त नई फसल होने पर और मांगी गई मुराद मन्नत पूरी होने पर विशेष रूप में किया जाता है। मुसाधा लोक गायन का आयोजन नई फसल होने पर लोक गायक घर-घर जाकर अपना गायन सुना कर भी नई फसल बधाई के रूप में प्राप्त करते हैं। मुसाधा गायन का आयोजन रात को खान पान से निवृत होकर शुरू होता है और सवेरे लगभग चार बजे तक जारी रहता है। जिस स्थान पर मुसाधा का आयोजन किया जाता है, उस स्थान को गाय के गोबर लीपा जाता है। लोक कलाकारों को आसन बिछाकर बैठाया जाता है और उनका भरपूर आदर सत्कार होता है। आयोजक अपनी इच्छा अनुसार बरसोद (पांच माणी अन्न) या दस्यूंद (10 माणी )भगवान के निमित्त करता है। सामर्थ्य अनुसार कई लोग तो भेड़ -बकरी भी भेंट में देते हैं। मुसाधा लोक गायक सर्वप्रथम अपने साजो को धुप दिखाकर गायन की शुरुआत करता है और फिर देखते ही देखते भक्ति रस की वो धारा बहने लगती, जिसमें श्रद्धालु मग्न हो जाते है। मुसाधा के वजूद पर संकट ! तकनीक के इस दौरे में कई पुरातन धार्मिक परम्पराएं आज ओझल होती प्रतीत होती हैं, जिनमे से मुसाधा भी एक है। एक दौर तय जब मुसाधा लोक कलाकारों का जमकर सम्मान होता था, पर वर्तमान में लोक संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर के वजूद पर संकट मंडराने लगा है। अब मुसाधा कलाकारों की संख्या बेहद कम रह गई है। जो इस परम्परा से जुड़े भी है उनके लिए भी जीवन यापन आसान नहीं। हालांकि समय -समय पर भाषा एवं संस्कृति विभाग विभिन्न आयोजन करता है, लेकिन ये प्रयास नाकाफी है।
हिमाचल प्रदेश में एक गांव ऐसा भी है जहाँ न तो मुर्गा पाला जाता है और न ही खाया जाता है। दरअसल ऐसा देव मान्यता के चलते है। चंबा जिला के भरमौर उपमंडल के एक दुगर्म गांव कुगती में कार्तिक स्वामी का मशहूर मंदिर है, जिसे केलंग बजीर से नाम से ख्याति प्राप्त है। मुर्गा देवता के झंडे में विराजमान है, जबकि मोर उनका वाहन है। इसलिए इस गांव में न तो मुर्गा पाला जाता है और न ही खाया जाता है। केलंग बजीर गद्दी समुदाय के अलावा कांगड़ा-चंबा और लाहौल-स्पीति के लोगों के ईष्ट देवता हैं। कार्तिक स्वामी भगवान शिव शंकर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिन्हें देवभूमि हिमाचल प्रदेश में केलंग बजीर के नाम से पूजा जाता है। पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान शिव भक्त इस मंदिर में पहुंच कर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। श्रद्धालु पवित्र डल की परिक्रमा करने के उपरांत कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं। जबकि लाहुल-स्पीति से कुगती होकर मणिमहेश यात्रा पर आने वाले शिव भक्त कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के बाद मणिमहेश पहुंचते हैं। सर्दियों में बर्फबारी होने के कारण नवंबर माह के आसपास केलंग बजीर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जो प्राचीन परंपरा के अनुसार अप्रैल में बैसाखी के दिन खोले जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद होने से पहले मंदिर में एक गड़वी (लोटा) में पानी भरकर रखा जाता है। जब मंदिर के कपाट दोबारा खुलते हैं, तो उस गड़वी में मौजूद पानी से यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला साल क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। यदि गड़वी में पानी कम मिलता है, तो यह सूखे की आशंका को दर्शाता है, जबकि पानी भरा हुआ मिलने पर सुख-समृद्धि की संभावना मानी जाती है। हर वर्ष जून माह में केलंग बजीर का जन्मोत्सव मनाया जाता है जो सात-आठ दिनों के लिए चलता है। इस दौरान कुगती पारंपरिक वाद्य यंत्रों से देवधुनों से अपनी अलौकिकता का अहसास करवाता है। इस बीच देवता के मंदिर में खेल का आयोजन भी होता है।
-प्रवेश के लिए लेनी पड़ती है इजाजत, नशेड़ियों के लिए गांव के दरवाजे बंद कुल्लू घाटी का एक ऐसा गांव जहाँ आज भी बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ तंबाकू, शराब और चमड़े से बनी वस्तुओं पर सख्त प्रतिबंध है। इस गांव का नाम है परभी, जिसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजोए रखा है। कभी पार्वती घाटी के मलाणा गांव में भी बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन अब वहां बाहरी लोगों को गांव में प्रवेश करने से नहीं रोकते हैं। पर वक्त के साथ भी परभी गांव के नियम-कायदे नहीं बदले। बर्फ से लकदक सफेद फुंगानी पर्वत के आँचल में बसे परभी गांव ने अपनी पुरातन जीवनशैली को संरक्षित रखा है। गांव में पारंपरिक काठकूणी शैली में बने घर मौजूद हैं, जिनकी बालकनियों में लकड़ी के छत्ते हैं। अनाज के भंडारण के लिए घरों के बरामदों में रखे बड़े लकड़ी के बक्से, घरों में देसी मधुमक्खी के लकड़ी के छ्ते और घरों के सामने एक लाइन से लटके हाथ से बुने हुए पारंपरिक कपड़े और पट्टू ; ये आपको एक अलग दुनिया में ले जाते है, मानो सदियों पहले यहाँ वक्त की सुई थम गई थी। यहाँ आटा पिसाई के लिए आज भी घराट का इस्तेमाल होता हैं। गांव में मंदिर के पास एक प्राकृतिक पेयजल स्रोत है ,जहाँ आज भी जूते पहनकर जाने की मनाही है। परभी गांव में एक पहाड़ी किले के अवशेष भी मौजूद है, जिसे परभी गढ़ के नाम से जाना जाता है। कहते है सदियों पहले कबीलों के स्थानीय सरदार पहाड़ की चोटियों पर निगरानी टावरों के रूप में ऐसे गढों का निर्माण करवाते थे। इस किले के अवशेष अब भी आपको अतीत में खींच ले जाते है। यहाँ के ग्रामीणों के लिए परभी गढ़ एक पवित्र स्थान है और ग्रामीण हर साल इस गढ़ की यात्रा करते हैं। गांव में मां फुंगणी का मंदिर है, जिसकी खास मान्यता है। परभी गांव अब तक सड़क से नहीं जुड़ा है। गांव तक पहुंचने के एक घंटे की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। कुल्लू से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव तक पहुंचने के लिए पहले कराल गांव पहुंचा जा सकता है। कराल गांव से खड़ी चढ़ाई के साथ परभी का रोचक सफर शुरू होता है। आसपास बर्फ से ढकी चोटियों के साथ ऊंचाई पर जाते -जाते कुदरत के नज़ारे और मनमोहक होते जाते हैं। बाहरी लोगों को गांव में प्रवेश करने से पहले ग्रामीणों से अनुमति लेनी पड़ती है। साथ ही गांव के बाहर लगे चेतावनी बोर्ड की पालना सुनिश्चित करनी होती है।
- आज भी समृद्ध कुल्लू की देव संस्कृति, सभी देवताओं के जगती स्थल हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ सनातनी संस्कृति की जड़े विधमान है। दुनिया की सबसे पहली मूर्ति हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थापित हुई थी, और संसार में पहली बार यहीं पर मूर्ति पूजा भी हुई थी। कई इतिहासकारों और लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। इसमें भी कोई संशय नहीं कि कुल्लू की देव संस्कृति बेहद समृद्ध है, और आज के दौर में भी हम यहाँ प्राचीन आर्यों के जीवन की एक झलक देख सकते हैं। कुल्लू को ठारह करड़ू का देश कहा जाता है। ठारह करडू की कहानी दिलचस्प है। प्रचलित अनुश्रुति है कि एक बार महर्षि जमदग्नि कैलाश की परिक्रमा करके स्पीति के रास्ते कुल्लू की ओर आ रहे थे। महर्षि अपने साथ एक टोकरी में अठारह देवताओं की प्रतिमाएं उठाए हुए थे। वे कुछ समय हामटा नामक स्थान पर ठहरे और फिर मलाणा की ओर बढे। इस दौरान जब वह चन्द्रखणी पर्वत पर पहुंचे तो प्रचंड हवा चली और टोकरी में रखी सभी प्रतिमाएं उड़ कर दूर- दूर जा गिरी। अनुश्रुति है कि जहां-जहां वे प्रतिमाएं गिरीं, वहां वे देवता रूप में प्रकट हो गईं। तब हर एक प्रतिमा के लिए एक अलग टोकरी बनी, जिसे कुल्लई ज़बान में करडू, करड़ी, करण्डी या कण्डी कहते हैं। राजनितज्ञ एवं प्रख्यात लेखक स्वर्गीय लाल चंद प्राथी अपनी पुस्तक 'कुलूत देश की कहानी में मूर्ति स्थापित होने के इस प्रसंग का उल्लेख किया है। प्राथी लिखते हैं कि इसी के साथ देवता जो इससे पूर्व निराकार था, कुल्लुत देश में मूर्ति के रूप में साकार हो गया और सम्भवत: सबसे पहले मूर्ति पूजा भी यहां शुरू हुई। लाल चंद प्रार्थी लिखते हैं कि जब प्राचीन आर्य ऋषि सप्त सिन्धु में रहते थे। जब वेदों की रचना हो रही थी, जब संसार में मूर्ति का कोई विचार तक नहीं था और वैदिक ऋषि प्रकृति की शक्तियों को ही निराकार देवता के रूप में मानते थे, तब कुलूत देश को महर्षि जमदग्नि ने अठारह प्रतिमाएं देकर इसे ठारह करडू का देश बना दिया था। कुल्लू में सभी देवताओं के कुछ पर्व एवं दिन निश्चित होते हैं, जिस दिन गूर या माली देवता के रथ या मूर्ति के सामने बैठकर समस्याओं का निवारण करता है। कुल्लू के सभी देवी-देवताओं के अपने-अपने जगती स्थल हैं। कुल्लू में लगभग सभी देवी-देवताओं के मंदिरों के बाहर एक चबूतरा बना होता है, जिसे थौल कहते हैं। देवता इस पर बैठता है। इसके सामने पटड़ी जो लकड़ी का फट्टा होता है, जिस पर बैठकर गूर लोगों की समस्याओं का निराकरण करता है। मान्यता है कि जब देवता का जन्मदिन होता है, देवता स्वर्गलोक से या देवयात्रा से लौटकर आता है, या कोई अन्य विशेष अवसर होता है, तब गूर जगती पर बैठकर अपना इतिहास सुनाता है और प्रजा की सुख-समृद्धि के उपाय बताता है। राजपरिवार का मुखिया करता है जगती पूछ का आयोजन जब कभी देश पर विकट संकट आता है मसलन प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भुखमरी आदि, तो नग्गर गांव में कुल्लू भर के देवता इकठ्ठे होते हैं, जिसे जगती पूछ कहते हैं। जगती पूछ का आयोजन कुल्लू के राजपरिवार का प्रमुख देवी- देवताओं के आदेशानुसार करता है और कुल्लू स्थित राजमहल से ठारह करडू का धड़छ मान सम्मान सहित परंपरानुसार इस स्थल पर लाया जाता है। सभी देवी-देवताओं के प्रतिनिधि गूर और पुजारी अपने-अपने देवताओं के घंटी और धड़छ लेकर इस पवित्र स्थान पर इकठ्ठे होते हैं। देवता यहां इकठ्ठे होकर जगत के कल्याण के लिये विचार-विमर्श करते हैं। यहां पर 5 इंच मोटा 6 फुट चैड़ा और 8 फुट लंबा पत्थर है जिसे जगती पौट कहते हैं। जनश्रुति है कि जगती पौट की इस शिला को कुल्लू के समस्त देवी-देवताओं ने मधुमखियों का रूप धारण कर भृगुतुंग पहाड़ी के एक छोटे से भाग द्राम ढोग से लाकर नग्गर में स्थापित किया था। कुल्लू दशहरे में होती है छोटी जगती कुल्लू दशहरे में भी छोटी जगती होती है। दशहरे में आए हुए देइ -देवता इसमें शामिल होते हैं। ये आयोजन भगवान रघुनाथ के शिविर में करवाया जाता है और इसमें नग्गर की देवी त्रिपुरासुंदरी, कोटकंढी के पंजवीर देवता तथा जमलू देवता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार बारी-बारी से सभी देवताओं के गूरों के पास जाते हैं और उनसे अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध करते हैं। सभी गूर एक-एक करके अपनी बात रखते हैं। आवश्यकता अनुसार कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में भी जगती पूछ का आयोजन होता है। 'कुलूत देश की कहानी' में लाल चाँद प्रार्थी ने लिखा है - " कुल्लू मान करता है अपनी प्राचीनतम संस्कृति पर, अपनी दंवी सम्पत्ति पर, अश्पनी उज्ज्वल परम्पराओं और अद्भुत लोक कलाओं पर, और उपयुक्त रूप से गर्व करता है उन अनुश्रुतियों पर जो उसने अपने हृदय में हज़ारों लाखों सालों से सुरक्षित रखी हैं......उस युग से जब अभी संसार की पहली पुस्तक ऋग्वेद भोजपत्र पर लिखी नहीं गई थी, जब मानव की कल्पना वैज्ञानिक शक्ति के प्रभाव में नहीं आई थी। हाँ ! कुल्लू कृतज्ञ है प्रकृति की उदारता का जिसने इसे यह भौगोलिक स्थिति प्रदान की, और जिस की अनुकम्पा से वह न्यूनाधिक सुरक्षित रहा उन सभी प्रभावों से जो हर दौर में बाहर के आक्रमण कारियों के कारण सप्त सिन्धु श्रौर पंजाब की सभ्यता को बार बार मिट्टी में मिलाते रहे। "